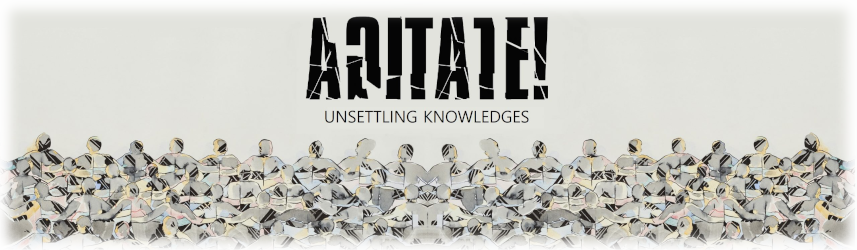इंसानियत का लॉकडाउन
ऋचा नागर और ऋचा सिंह
Richa Nagar and Richa Singh
This article was originally published by Junputh on April 18, 2020.
The title of this piece, by Richa Nagar and Richa Singh, translates to—Humanity in Lockdown. It emerged from notes exchanged between the two authors during March and April of 2020 across Minnesota in the Midwestern United States and Sitapur District in the Northern Indian state of Uttar Pradesh soon after Prime Minister Narendra Modi announced on 23 March 2020 at 8pm that India, a country of more than one-billion, would go into a nation-wide lockdown within four hours. The lockdown order made no provisions for the thousands of migrant workers, predominantly from Dalit and other marginalized communities, who labor in factories, stores, and as domestic help in India’s megacities, hundreds of miles away from their homes. With no assurances about their safety or survival, migrant workers gathered their belongings into a few bags and began the journey back to their villages. They thronged bus stations such as Anand Vihar at the Delhi-Uttar Pradesh border, hoping to board a bus. Given the near impossibility of finding transport in the chaos of those days, many undertook the journey on foot, walking on endless highways without food or water, carrying their belongings and their hungry children upon their shoulders. The harassment that many suffered at the hands of the police and health officials tasked with enforcing the lockdown during their treacherous journeys, will shock even the strongest among us.
Nagar and Singh explore the implications of this ill-planned lockdown through the experiences of their comrades in the Sangtin Kisan Mazdoor Sangathan who live in Sitapur District of Uttar Pradesh. What emerges are lockdown stories that show the intersections of economic deprivation and hunger, and the isolation of Muslims in local communities. In Sitapur, they write, many Hindus refuse to even buy vegetables from Muslim vendors. More recently, Hindu religious festivals have become occasions to terrorize and threaten Muslims openly. Here we republish this article, with a new introduction written for this volume.
6 मई 2022
दो शब्द, दो साल बाद
जो लेख आप पढ़ने जा रहे हैं वह हमने मार्च-अप्रैल 2020 के भयावह दौर में मिनिसोटा और सीतापुर के बीच के फ़ासले जीते और मिटाते हुए लिखा था। उस वक़्त कोरोनावायरस के महामारी बनने और प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर लॉकडाउन जारी होने के साथ ही भारत-भर के प्रवासी मज़दूर शहरों से अपनी पूरी-की-पूरी ज़िंदगियों को दो-तीन गठरियों और बस्तों में बटोरकर और उन्हें अपनी पीठ पर लादकर अपने घरों और गाँवों की तरफ़ वापस चल दिए थे। उन्हें डर था कि जिन शहरों को वे अपने ख़ून-पसीने से सींचते हैं वहां उन्हें जाति-धर्म-वर्ग के आधार पर पराया बना दिया जायेगा और अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनका कोई पुरसाहाल नहीं होगा। मज़दूर साथियों की वापसी के उस दर्दनाक मंज़र पर न जाने कितने गीत-कविताएं और निबंध रचे गये।आज भी उन दृश्यों को याद करते हुए रोंये सिहर उठते हैं।
लेकिन कुछ ही महीनों बाद मज़दूर साथी उन्हीं शहरों की ओर वापस लौटने लगे जिन्होंने उनसे मुँह मोड़ा था। वह मज़दूर साथी क्यों और किस हाल में लौटे या अभी भी लौट रहे हैं उस तरफ़ किसी ने ज़्यादा तवज्जोह नहीं दी। वक़्त भी कहाँ था, क्योंकि महामारी का एक साल पूरा होते-होते डेल्टा वैरिएंट ने इस तरह मुँह उठाया कि गंगा मैया ही शव-वाहिनी बन गयी। अप्रैल और मई 2021 में कोविड के लाखों मरीज़ों ने आक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया। हस्पतालों में भर्ती कितने ही मरीज़ अपने बग़ल के बिस्तर पर दूसरे मरीज़ को तड़प-तड़प कर मरता हुआ देखते और फिर उस मृत मरीज़ का शव उसी पलंग के नीचे डाल दिया जाता और दूसरा मरीज़ उसी बिस्तर पर लेटा होता। शमशान घाटों पर मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ियों का अकाल पड़ गया, और कितनों को कफ़न ही नसीब नहीं हुआ। पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसका कोई प्रियजन महामारी की भेंट न चढ़ा हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन के मुताबिक़ 2020 और 2021 में भारत के 47.4 लाख लोग कोविड से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मरे हैं जबकि भारत सरकार अभी भी 2021 के अंत तक मरने वालों की संख्या 4.81 लाख बता रही है।
अप्रैल 2020 के लॉकडाउन के दौरान तबलीग़ी जमात के सम्मलेन के बहाने भारतीय नेताओं और मीडिया ने कोरोना वायरस को मुस्लिम समुदाय से फैलने वाली बीमारी बना दिया था। महीनों तक हवालात में बेवजह बंद किये गए तबलीग़ी जमात के लोग भले ही अब तक रिहा हो गये हों, लेकिन क़ौमी नफ़रत को गहराने का काम तो उसी वक़्त बख़ूबी संपन्न हो गया। सीतापुर के गांवों में कितने ही हिन्दुओं ने अपने परिचित मुसलमान साथियों से सब्ज़ी तक लेने से इंकार कर दिया। इस तरह की दूरियां बहाने-बहाने से बढ़ती-ही चली जा रही हैं, साथ ही खुल्लमखुल्ला ज़हर फैलाने का काम भी। पिछले माह नवरात्रि पर शोभायात्रा के बहाने मस्जिदों के सामने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाती भीड़ों को आख़िर किस नाम से पुकारा जाये? सीतापुर ज़िले के ख़ैराबाद में ऐसी ही एक शोभायात्रा हैवानियत की हदें पार कर गई जब एक भगवाधारी ने ऐलान किया कि अगर हमारी बहन बेटियों को छेड़ा तो हम मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करेंगे, और यात्रा में शामिल कितने ही युवा ‘जय श्री राम’ का उदघोष करते हुए ताली बजाकर झूम उठे।
क़ौमी नफ़रतों और अविश्वास का ज़हर आग की तरह फैल रहा है। संगतिन किसान मज़दूर संगठन में हम एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए अक्सर एक कहानी सुनाते रहे हैं: हमारे जंगल में आग लगी है, और उस आग को बुझाने के लिए एक नन्हीं-सी चिड़िया अपनी चोंच से पानी ला-लाकर डाल रही है, जबकि एक ताक़तवर हाथी अपनी लम्बी-सी सूंढ़ में पानी भरकर आग बुझाने के बजाय दूर खड़ा सिर्फ़ तमाशा देख रहा है। चिड़िया को मालूम है कि जब जंगल का इतिहास लिखा जायेगा तब उसकी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, दूर से तमाशा देखने वालों में नहीं। लेकिन अब लगता है मानो हमारी यह कहानी थक रही है–आग बुझाने वाली चिड़िया के पंख झुलस रहे हैं और दूर से ताली बजाने वाले तमाशबीनों की तादाद बढ़ती जा रही है। जंगल में लगी आग की तपिश अब हमारे घरों के दरवाज़ों में ही नहीं, बल्कि हमारे घरवालों के मनों में भी धंस चुकी है। अगर जंगल नहीं बचा तो घर कहाँ से बचेगा? मन कहाँ से बचेगा? और फिर चिड़िया की नज़र से लिखा इतिहास भी कितना बच पायेगा? जंगल को बचाने के लिए इस वक़्त अनगिनत चिड़ियों की ज़रुरत है।
18 अप्रैल 2020

मार्च 2020 में जैसे-जैसे पूरा मानव संसार कोरोना वायरस की चपेट में अपनी-अपनी सरकारों के लॉकडाउन ऑर्डरों के भीतर बंद होता चला गया, सबके डर बढ़ते गए- “क्या होगा हमारा और हमारे प्रियजनों का?” चीन, इटली, और स्पेन की तो जाने दो, जब अमरीका में COVID-19 इतना क़हर बरपा रहा है तो उत्तर प्रदेश के गांवों की क्या बिसात? वही उत्तर प्रदेश, जहां आज भी कितने ही ग़रीब लोग तपेदिक और टिटनेस से मर जाते हैं। जहां के अस्पतालों में आक्सीजन की कमी से एक ही दिन में ढेरों बच्चों की मौत हो जाती है। जहां एक्सपायर हो गयी दवाइयों के असर से आज भी लोग दम तोड़ देते हैं!
कई ने अपनी और अपनों की जान की चिंता करने के साथ-साथ गहरे सवाल भी खड़े किये उस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर, जिसके स्वार्थ और हवस में से इस कोरोना वायरस और इससे पहले वाले कोरोना वायरसों का जन्म हुआ। तमाम लोगों ने इतिहास में गुज़री ऐसी ही बीती विपदाओं और 1918 के स्पैनिश फ़्लू जैसी महामारियों को याद किया जिन्होंने आज से दशकों पहले दुनिया के करोड़ों लोगों को निगल लिया था।
इन संवेदनशील चर्चाओं को सुनते-समझते चन्द पलों के लिए ऐसा लगा मानो मुख़्तलिफ़ दुनियाओं में बसे लोगों के ग़म आपस में अचानक इस क़दर गुँथ गये हैं कि इस नये कोरोना वायरस से उपजी आपदा सिर्फ़ इंसान को इंसान से नहीं बल्कि जीव-जंतुओं और प्रकृति से भी एक नयी गहराई के साथ जोड़े दे रही है- कदाचित एक ऐसे रिश्ते में, जहां हम प्रकृति में जी रही हर सांस के साथ एक न्यायपूर्ण और नैतिक रिश्ता बना सकें। क्षण-भर को यह भ्रम भी हुआ मानो इस महामारी की दहशत दुनिया के सारे शासकों को अपनी इंसानियत को फिर से पाने के लिए (या जो शेष रह गयी है उसे बचाने के लिए) प्रेरित कर रही हो और शायद इसी वजह से सब के सब अपनी-अपनी प्रजाओं के लिए लॉकडाउन का आदेश जारी कर रहे हैं।
लेकिन हमारी सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्था में अगर इतनी बुनियादी इंसानियत होती तो इस लॉकडाउन में अनगिनत इंसानों और इंसानियत का दम वैसे नहीं घुटता जैसे इस वक़्त घुट रहा है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च की रात 8 बजे एलान किया कि देश के एक अरब तैंतीस करोड़ से भी अधिक लोग कुल चार घंटों के भीतर लॉकडाउन में भेज दिये जाएंगे क्योंकि देशवासियों को बचाने का एक यही तरीक़ा है। कहां तो 30 जनवरी को देश में COVID-19 का पहला केस सामने आने के बाद भी अनगिनत रूपये और संसाधन डॉनल्ड ट्रम्प की आवभगत में लगाये जा रहे थे और कोरोना वायरस को मज़ाक ठहराया जा रहा था, और कहां रातों-रात लॉकडाउन के आदेश!
आदेश सुनते ही असंख्य लोग हक्के-बक्के रह गए। इसलिए नहीं कि उन्हें इस बात पर संदेह था कि देश के लोगों की जान बचाने का यह असरदार तरीक़ा हो सकता है, बल्कि इसलिए कि जिस आदेश को इतनी तेज़ी के साथ एक ही झटके में पूरे देश पर लागू कर दिया गया, उसकी तैयारी लगभग न के बराबर थी। जो लोग प्रधानमंत्री द्वारा इतने बड़े क़दम उठाने की तारीफ़ करने में लगे थे उन तक के दिलो-दिमाग़ में दर्ज़नों सवाल कौंध गए- क्या-क्या बन्द होगा? और बन्द करने से पहले सरकार क्या-क्या सोचेगी? जो लोग सरकार से नाउम्मीद बैठे हैं, उन्होंने घबराकर यह भी पूछा- क्या इस लॉकडाउन को लागू करते हुए हमारे तथाकथित रहनुमाओं की नज़र हाशिये पर धकेले गये लोगों तक पहुंचेगी?
सामाजिक न्याय से जुड़ी कितनी ही चर्चाओं में बरसों से यह बात उठती रही है कि दलित मज़दूरों और किसानों के साथ खड़े होने का मतलब है कि हमें हाशियों को ही केन्द्र बनाना होगा। लेकिन हाशियों को केन्द्र बनाना तो दूर, यहां तो यह भी नहीं सोचा गया कि रातों-रात लॉकडाउन होने से अपने घरों-गांवों से सैंकड़ों मील दूर-दराज़ के शहरों, कारख़ानों, दुकानों में अपने मालिकों की हाज़िरी बजाकर अपनी रोज़ी-रोटी चलाने वाले प्रवासी मज़दूर कैसे इस आदेश को अंजाम देंगे? वे मज़दूर जिनके पसीने से हिंदुस्तान का ब्राम्हणवादी पूंजीवाद चलता है, उनकी हिफ़ाज़त कैसे होगी?
यह सब सोचना शायद हमारे शासकों के लिए मुमकिन था ही नहीं। नतीजतन, जो भयावह दृश्य आनन्द विहार बस अड्डे पर पहले पहल दिखा लगभग वही दृश्य बार-बार देश भर में दोहराता चला गया। अंतहीन रास्तों पर अपना सामान लादे पैदल चल रहे मज़दूरों की कभी न ख़त्म होने वाली कतारें, थकन और भूख से बेकल लोगों के झुण्ड-दर-झुण्ड, उनके कन्धों पर बैठे या उनकी बांहों में समाये भूख-प्यास से बेदम होते बच्चे।
उससे भी भयानक थी इन मज़दूर साथियों के साथ हो रही अकल्पनीय बर्बरता जिसकी सोशल मीडिया में घूमती तस्वीरें और वीडियो देखकर मज़बूत से मज़बूत कलेजे वाला भी अपनी आँखें बंद कर ले। बदायूँ में पुलिस ने घर जाते मज़दूरों को “अनुशासित” करने के लिए लाठियों की नोक पर उन्हें कान पकड़कर पीठ पर लदे सामान के साथ मेंढक की तरह सड़कों पर कुदवाया। बरेली में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने घर लौटते मज़दूरों को वायरस से मुक्त करने के लिए उन पर सोडियम हाइपोक्लोराइट यानी ब्लीच में इस्तेमाल होने वाले रसायन का छिड़काव करना ज़रूरी समझा। पूर्वी बिहार में दर्ज़नों मज़दूरों को लॉकडाउन के तहत सलाख़ों के पीछे कर दिया गया और पश्चिम बंगाल सहित न जाने कितने इलाक़ों में घर लौटते मज़दूरों को गांवों के भीतर दाख़िल होने से रोक दिया गया।
लेकिन इन दर्दनाक दृश्यों का बखान करके वहीं रुक जाना काफ़ी नहीं है- हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ज़रा इनकी तहों में जाकर झांकें ताकि थोड़ी और गहराई से समझ सकें कि बिना तैयारी के इस लॉकडाउन की क़ीमत कौन और कैसे चुका रहा है। इन तहों में पहुंचने के लिए हम सीतापुर ज़िले के गांवों में काम कर रहे संगतिन किसान मज़दूर संगठन के जुड़े अपने साथियों के अनुभवों का सहारा लेते हैं।
पेट का लॉकडाउन?

लॉकडाउन का मतलब देश के मज़दूर साथी तुरंत समझ गए- काम बन्द और कमाई बन्द! लेकिन पेट कहां बंद होता है? पहले सवाल यही थे- कहां से अपना पेट चलाएंगे और कहां से परिवार को खिलाएंगे? जब शहरों के नौकरीपेशा लोग अपने-अपने घरों में बंद होने की तैयारी करने में जुटे, तब रोज़ी-रोटी की तलाश में अपने-अपने गांवों से सुदूर शहरों में पसीना बहाते मज़दूर सड़कों पर आ गए। जहां देश का एक हिस्सा राशन और रोज़मर्राह की चीज़ें ख़रीदने के लिए दुकानों में लगी लाइनों में खड़ा हुआ वहीं कई करोड़ प्रवासी मज़दूरों ने अपने बड़े-बड़े जिगरों और नन्ही-नन्ही गृहस्थियों को बैगपैक, झोलों, और छोटी-बड़ी गठरियों में समेटकर तथा अपने बच्चों को कन्धों पर बिठाकर अपने गांवों की ओर रुख़ किया।
क्या सोच कर लोग यों निकल पड़े? यही न, कि जहां काम कर रहे हैं वहां हमारा कौन है? कौन खड़ा होगा इस महामारी में हमारे साथ? अगर मज़दूरों के हक़ों और हित के लिए पहले से ही एक मानवीय व्यवस्था बनी होती जिसमें से जातिवाद और वर्गवाद की भयंकर दुर्गन्ध न आती तो क्या यों करोड़ों लोग निकल पड़ते सड़कों पर?
लेकिन जब गाज गिरी तो मज़दूर ही थे जो हिम्मत कर सकते थे दर्ज़नों, सैंकड़ों किलोमीटर के सफ़र पर यों निकल जाने की! दलित-आदिवासी-ग़रीब मज़दूरों की ज़िन्दगियों का मूल-मंत्र यही तो है कि “पैदा हुए हैं तो रोटी भी मिल ही जाएगी।” “जब तक आस है, तब तक सांस है।” “सब्र करो, सब दिन एक समान नहीं होते।” ऐसी ही कितनी कहावतें और सीखें जो पल-पल की कठिन ज़िन्दगी को जीने की राह देती हैं।
पिछले कई बरसों से लगातार खाली हो रहे गांव तो हम सब ख़ूब देख रहे थे। अपनी चर्चाओं में हम अक्सर ग़ौर करते कि ग्रामीण इलाक़ों से इतने बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है कि गांव एक के बाद एक लगभग ख़ाली होते चले जा रहे हैं। लेकिन भारत के गाँवों में किस हद तक नाउम्मीदियों का सन्नाटा छाया है यह तो 24 मार्च के तुरंत बाद ही समझ में आया। संगठन की साथी बिटोली के अक्सर दोहराये शब्द कानों में बार-बार गूँजने लगे- “हम दलित मज़दूरों की ज़िन्दगी तो कीड़े-मकोड़ों की तरह है।” क्या हमारे शासकों को ऐसे ही दीख रहे थे सड़कों पर चलते हुए असंख्य मज़दूर साथी?
इन्हीं अनगिनत साथियों में से एक चलते-चलते गिर पड़ता है। COVID-19 उसकी सांसों से खेलने की ज़ुर्रत करे, उससे बहुत पहले ही उसकी सांसें लॉकडाउन के क़हर में थम जाती हैं। उसके आधार कार्ड से मालूम होता है कि वह मध्य प्रदेश के एक गांव का था। उसकी तस्वीर फेसबुक, ट्विटर, और व्हाट्सएप पर इधर से उधर घूमती है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक अन्य मज़दूर की जो अपनी पत्नी को कंधे पर लेकर चल रहा था क्योंकि उसका पैर टूटा था। कहां होगा वो शख़्स इस वक़्त? अपने घर तक पहुँच पाया होगा या उससे पहले ही कहीं लड़खड़ाकर गिर गया होगा? इसी तरह घूमता है उस औरत का चित्र भी जिसके मज़दूर पति को कार कुचलकर निकल गयी थी और वह अपने जीवन साथी की लाश गोद में लिए बैठी थी। सोशल मीडिया पर मंडराती ऐसी कितनी ही दर्दनाक तस्वीरों और तथ्यों के बीच मज़दूरों और उनकी मौतों के आँकड़े बढ़ रहे हैं- अंतहीन कतारों में रेंगते बिन नामों के आँकड़े।
पिसावाँ के बिचपरिया गांव की एक साथी का सुबह फ़ोन आता है- उसका 18 साल का बेटा अपने दोस्त के साथ दिल्ली में है। काम बन्द हो चुका है। दो दिन का खाना है। वापसी के लिए न तो कोई साधन है न ही पैसे।
मछरेहटा ब्लॉक के गांव पहलीपुरवा के चार लोग लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर पैदल चलकर सिधौली पहुंचते हैं और परिजन उन्हें सिधौली जाकर बाइक से घर लाते हैं। जहां असंख्य ठिकानों से लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित घरों के लिए पैदल चल पड़े हों, वहां पचास किलोमीटर क्या मायने रखता है?
मछरेहटा के ही एक और गांव से दो युवा मज़दूर अपने मालिक से सायकिल मांगकर चल पड़ते हैं। एक्सिडेंट होता है और उनमें से 19 साल के एक मज़दूर की तुरंत मौत हो जाती है। काम बन्द होने पर मज़दूर घर कैसे जाएंगे? सरकार के लिए यह पहले से सोच पाना क्या इतना कठिन था? अगर एकाध दिन का समय हाथ में होता तो वे नौजवान जो सायकिल से चल पड़े, यों कभी नहीं चलते।
हम संगठन में अक्सर देखते-सुनते थे कि फ़लाने का लड़का बाहर कमाने गया है, या फ़लाने का बेटा किसी बात पर रूठकर दिल्ली चला गया। गांव छोड़कर निकले ये नौजवान कहीं रिक्शा चलाते हैं, कहीं ईंट-मिट्टी-गारा ढोते हैं, किसी की फ़ैक्टरी में लग जाते हैं, या वर्दी पहनकर किसी कारख़ाने का गेट खोलने और बन्द करने का काम करते हैं। एक नज़र में ये सारे युवा साथी कमोबेश एक से दीखते हैं- पैरों में विदेशी ब्रांडों का नकली नाम धरे जूते, जीन्स पहने, कानों में हेडफ़ोन की लीड, हाथ में चाइनीज़ मोबाइल और पीठ पर बैगपैक। बैग तो इनके वैसे भी अक्सर ख़ाली ही होते हैं, लेकिन इस मार्च में जब ये वापस घर लौटे हैं तो और भी बहुत कुछ लाए हैं अपने साथ- पैरों में छाले, सूखे मुंह और होंठ, ख़ाली पेट और दिलो-दिमाग़ में ऐसे सदमे जिनका कभी कोई डायग्नोसिस नहीं होगा। कोई पुलिस की लाठी की मार को याद करके रात की नींद में बार-बार चीख़ता है तो कोई अपने इर्द-गिर्द की भूख, पीड़ा, और दहशत को याद करके बिलकुल सुन्न हो जाता है या बेतरह बिलखने लगता है।
इस सबके बीच पहली अप्रैल से शुरू हुआ वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं का क्रियान्वयन और फिर राशन वितरण। लेकिन तमाम परेशान करने वाले सवाल हैं- जैसे, लॉकडाउन से पहले मनरेगा की बक़ाया मज़दूरी और सामग्री के पैसों का भुगतान क्यों नहीं हुआ? जो काम सरकार आराम से कर सकती है, वे काम देश को बंद करने से पहले क्यों नहीं कर सकी?
जब तथाकथित शिक्षित और ख़ुद को मज़दूरों से ऊँचा मानने वाले समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी आँखों के सामने हो रहे अत्याचारों को देखने से साफ़ इंकार कर देता है तो सरकार से सवाल करना तो दूर की बात है। वह तो मज़दूरों को अपने गांवों की ओर वापस लौटता देखकर ही कुलबुलाने लगता है- “यह लोग वापस क्यों आ रहे हैं? अगर इनमें कोई COVID-19 पॉज़िटिव हुआ तो? अगर हमारे गांवों और बस्तियों में इनकी लायी महामारी फैल गयी तो?”
धर्म-जाति-वर्ग की भयानक सत्ता में पली यह कैसी ऊँचाई है जहां बैठकर इंसान इंसानियत से इतनी बेरुख़ी कर लेता है कि उसके मन को तमाम अहम सवाल नहीं मथते- जैसे, आनन्द विहार बस स्टेशन तक इतने सारे प्रवासी मज़दूर क्यों पहुँचे थे और वे सैकड़ों किलोमीटर की दूरियां नापने पैदल क्यों चल दिए? “ऊँचाई” पर बैठा यही तबक़ा महामारी को लेकर रोज़ सुबह जब अपनी ख़ैर मनाता है तो यह सोचकर क्यों नहीं तड़पता कि क्या बीती होगी उन पर जो चले तो थे घर के लिए लेकिन जिनकी सांसें बीच राह में ही थम गयीं हमेशा के लिए? कि जिन मज़दूरों ने भूख-प्यास-टूटन के मारे रास्ते में ही दम तोड़ दिया उनके परिवारों के क्या हालात होंगे? दूर-दराज़ के घरों-मोहल्लों में कौन लोग उनका इंतज़ार कर रहे होंगे?
इसी उथल पुथल के बीच हुई चर्चाओं के दौरान कई परेशान करने वाली बातें सुनाई देती हैं। शहर में रहने वाले एक परिचित आनन्द विहार को इटली को जोड़ते हैं – “इटली में अगर एक बुज़ुर्ग और एक युवा दोनों की हालत चिंताजनक है और केवल एक को ही बचाया जा सकता है तो वहां युवा को बचा रहे हैं।” लेकिन युवाओं का ज़िक्र जैसे ही बात को भारत के नौजवान प्रवासी मज़दूरों पर लाता है, वैसे ही वे कहते हैं- “लगभग 29 लाख लोग होंगे जो लॉकडाउन की वजह से भूखे होंगे, लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में यह कोई बड़ा आँकड़ा नहीं है।” इसके बाद नवरात्रि के व्रत का उदाहरण देते हुए यह भी कहते हैं कि “मज़दूर दो दिन भूखे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे!”
एक सवर्ण परिवार में जन्मा, पढ़ा-लिखा अच्छी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त व्यक्ति कितनी आसानी से व्रत को भूख से जोड़ गया! ऐसा व्यक्ति जो बस उस भूख से परिचित है जो रोज़ आती है और जब तुरंत खाने को नहीं मिलता तो और सताती है, लेकिन जो स्वयं उस भूख की कल्पना तक नहीं कर सकता जिसके आगे हमारे कितने ही मज़दूर साथी कई-कई दिनों और हफ़्तों के लिए असहाय हो जाते हैं। और वही व्यक्ति जब एक आंकड़े का सहारा लेकर ग़रीब, दलित, आदिवासी, और मुस्लिम मज़दूरों के प्रति हो रही प्रशासनिक और सामाजिक अमानवीयता को एक सांस में झुठला देता है तो इस सवाल का जवाब भी ख़ुद-ब-ख़ुद मिल जाता है कि लॉकडाउन की घोषणा होते ही तमाम शहरों से लोग वापस गांवों की तरफ़ क्यों चल पड़े।
ज़हर के बीच जगमगाहट

Migrant workers and their family members line up outside a New Delhi bus terminal hoping to board a bus for their villages. Millions have lost their ability to earn an income because of the government-imposed lockdown aimed at limiting the spread of the coronavirus.
बीते 5 अप्रैल को जब संगठन के एक मुस्लिम साथी से उनके राशन मिलने की बात चली, तो वे बोले, “मैं तो एक दिन भी बाहर नहीं निकला। घर में लोग क्या खा-पी रहे हैं यह तो हम ही जानते हैं। आज बारह-पंद्रह बरस के दो बच्चे मेरे सामने से बतियाते हुए गुज़र रहे थे। मुझे देखकर फुसफुसाए “ये जो कोरोना है न, इन्हीं मुसलमानों का लाया हुआ है!””
मार्च में दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीग़ी जमात का जो सम्मलेन हुआ उससे कोरोना वायरस को भारत में फैलने में कैसे मदद मिली, यह बात तो देश के हर नागरिक की ज़ुबान पर सुनायी दे जाएगी लेकिन इस पूरे मामले में भारत सरकार की लापरवाही ने क्या भूमिका निभायी है इस प्रश्न पर गहरी ख़ामोशी क्यों रही? इसीलिए न क्योंकि तबलीग़ी जमात के बहाने मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत का ज़हर फैलाने का एक ज़बरदस्त अभियान छेड़ा जा चुका है! मुस्लिमों को “कोरोना बम” की संज्ञा देकर और नक़ली वीडियो दिखा-दिखा कर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया ने एलान कर दिया है कि हिन्दुस्तान में कोरोना वायरस जान-बूझ कर मुस्लिम लाये हैं। फ़रवरी में दिल्ली में मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाकर जो हैवानियत घटी उसको बीते बमुश्किल एक माह गुज़रा होगा कि मुसलमानों को देशद्रोही क़रार करने की एक और भयानक साज़िश! ऐसा नहीं है कि घृणा की इस ख़तरनाक़ आग पर पानी के छींटें डालने का काम नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग यह ज़रूरी काम कर रहे हैं, उनकी पहुँच आग फैलाने वाली बड़ी-बड़ी मीडिया-कम्पनियों की अपेक्षा बहुत कम है।
और इसी के बीच लौटा टी.वी. सीरियल ‘रामायण’ और साथ ही आई 5 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित दीपोत्सव की रात। सीतापुर शहर में एक साथी के पूरे मोहल्ले में घरों की बत्तियां बुझी थीं, सिर्फ़ एक उसका घर छोड़कर। बाहर मोमबत्तियों, दीपकों और मोबाइल टॉर्चों की रोशनी हर जगह फैली हुई थी। ख़ूब शोर-गुल और गूँजते हुए ठहाकों के माहौल में “कोरोना गो” के साथ-साथ “भारत माता की जय,” “वन्देमातरम,” और “जय श्री राम” के नारे लग रहे थे और पटाख़े फूट रहे थे। अगले रोज़ उस साथी ने अपनी डायरी में लिखा-
“मेरे पड़ोसी भी अन्दर-बाहर की सभी बत्तियाँ बुझाकर मोमबत्ती हाथ में लिये खड़े थे। मेरा घर और मैं इस भीड़ में अकेले थे। एक पल को मुझे मेरा ही घर खटका। मेरे घर के अन्दर और बाहर रोशनी फैली हुई थी, रोशनी से तो कभी डर नहीं लगा था पर उस एक पल में मैं डर गयी। कहीं से कोई आकर यह न कह दे कि बत्ती बन्द कर दीजिए… फिर सोचा, मैं क्यों डर रही हूं? प्रतीकात्मक ही सही मैं अपना विरोध दर्ज कर चुकी थी। लेकिन मैं यह विरोध दर्ज कर पायी क्योंकि मैं एक सवर्ण परिवार से हूं और मेरे पैर मज़बूती से ज़मीन पर खड़े हैं। वरना इस अकेले घर में रहने वाली एक महिला के लिए क्या यह सम्भव था? . . . लेकिन दीपोत्सव को लेकर मेरे एक क़रीबी परिजन की प्रतिक्रिया मुझसे बहुत अलग थी, उनका कहना था- “दुखों को उत्सव में बदलना तो कोई मोदी जी से सीखे।””
संगतिन किसान मज़दूर संगठन के साथ चलते हुए हमने यह ख़ूब जाना है कि जब तमाम दीपशिखाएं एक साथ जलती हैं तो उस सामूहिक लौ से कितनी ऊर्जा मिलती है। तमाम कठिन लड़ाइयों में साथी जब थकने लगते हैं तब हम सब हाथों में मोमबत्तियां लेकर जाते हैं- कभी गांधी पार्क तो कभी बाबा साहेब आंबेडकर पार्क। बाबा साहेब और गांधीजी के संघर्षों को याद करके अपने संघर्ष के लिए नयी हिम्मत बटोरते हैं। लेकिन 5 अप्रैल को हमारी साथी के घर के आगे दीपोत्सव कार्यक्रम मनाते हुए शोर मचाता हुआ वह समूह क्या अपने देश और दुनिया में कोरोना से हो रही मौतों से जूझने की ताक़त अपने अन्दर महसूस कर पाया होगा? बिल्कुल नहीं! वरना उस उन्माद को सुनकर उस साथी को डर क्यों लगता? ज़्यादातर लोग तो यह सोच ही नहीं रहे थे कि वे जो कर रहे हैं वो है किसलिए (सिवाय इसके कि “मोदी जी ने कहा है इसलिए करना है”)। यह भी पता चला कि पुलिस रात साढ़े आठ बजे से ही कई क़स्बों की बत्तियाँ बुझवाने लगी थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने मोमबत्तियां इस भय से जलायीं क्योंकि न जलाने पर लोग कहते, “तुम ग़द्दार हो।”
कहां चली गयी हमारी संवेदनशीलता? जिस देश में हम वसुधैव कुटुम्बकम का नारा लगाते हैं, जहां घर में किसी की मृत्यु होने पर तमाम परिवार एक बरस तक कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, आज उसी समाज में दीपोत्सव मनाते हुए हम कैसे भूल जाते हैं कि बाक़ी दुनिया तो दूर, भारत में ही कोरोना वायरस और उससे जुड़े लॉकडाउन के कारण कितने ही लोग मौत की भेंट चढ़ चुके हैं।
हम सब जानते हैं कि कोई मौत जब एक आँकड़े के रूप में सामने आती है तो हमें कम झकझोरती है; लेकिन जब वही मौत हमारे जाने-पहचाने चेहरों और नामों के साथ जुड़ती है, जब हम अपनी ख़ुद की ज़िंदगियां उस ज़िंदगी में उलझी पाते हैं जो गुज़र गयी, तभी वो हमें गहरे तक हिलाती है। COVID-19 एक ऐसी महामारी है जो अमरीका और हिंदुस्तान में, ग़रीब और अमीर में, सवर्ण और दलित में, हिन्दू और मुस्लिम में भेद नहीं करती। फिर क्या वजह है कि हमारे देश का एक वर्ग जब आनन्द विहार बस अड्डे की भीड़ को देखकर घबराता है तो उस भीड़ में खड़े इंसानों की भूख-प्यास और कोरोना वायरस से उनकी हिफाज़त की फ़िक्र नहीं करता , बल्कि खीझते हुए बोल पड़ता है- “क्या कर रही है हमारी सरकार? ये लोग जहां पहुँचेंगे वहीं महामारी फैलाएंगे।” कुछ ने तो प्रवासी मज़दूरों तो बीमारी फैलाने वाला “मानव बम” तक बना दिया। कैसी दुखद विडम्बना और दोहरापन है- कोई ग़रीब जब प्रधानमंत्री के आदेश पर अपनी झोपड़ी में दिया जला दे तो वह राष्ट्रभक्त, और उसी ग़रीब को प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का पालन करते हुए आनन्द विहार की भीड़ में खड़ा हो जाना पड़े तो वह मानव बम!
अमरीका में जिस वक़्त 2.2 करोड़ से भी अधिक लोग अपनी जीविका खो चुके हैं और COVID-19 से मरने वालों वालों की संख्या 31 हज़ार के ऊपर पहुँच गयी है, उस दौर में मिनिसोटा जैसे तथाकथित शांत प्रान्त में लोगों द्वारा बदूकों की ख़रीद सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जिस समय अमरीका के डॉक्टर और नर्सें हिफ़ाज़त से अपना काम करने के लिए बार-बार मास्क की दरकार कर रहे हैं उस वक़्त सुनने में आता है कि अमरीका ने लाखों मास्क चीन से इज़राइल की सेना को मुहैया करवाये हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन आदेश के साथ ही ख़बर मिलती है कि भयंकर महामारी के इस काल में भारत के शासक अपनी जनता के लिए मास्क या वेंटीलेटर जैसे उपकरणों की जगह अपनी सेना के लिए इज़राइल से करोड़ों डॉलर की मशीन गनें ख़रीदने की तैयारी कर चुके हैं।
लेकिन मन को तोड़ देने वाली इन्हीं ख़बरों के बीच ऐसी भी कई सुर्ख़ियाँ आँखों के सामने से गुज़र जाती हैं जो थोड़ी-सी राहत और उम्मीद देती हैं- जैसे, केरल और क्यूबा की सरकारों और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा COVID-19 के हर मरीज़ की रक्षा के लिए किया जा रहा समर्पित काम। जैसे, ईरान के विरूद्ध अमरीका द्वारा लगाए प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ तमाम लोगों का जगह-जगह से मिलकर आवाज़ उठाना। जैसे, भारत के मज़दूरों द्वारा महामारी से जुड़े राशन वितरण के लिए एक सिलसिलेवार ढंग से काम करना। जैसे, भारत के तमाम लोगों का मिल-जुल कर मज़दूर साथियों के लिए खाने का इंतज़ाम करना।
जिस ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी समाज का पूरा ढांचा जातपात और मज़हबी छुआछूत में सदियों से सांस ले रहा हो, और जहां साधन-संपन्न वर्ग और साधन-विहीन वर्ग के बीच की लड़ाई भी इसी ढांचे के नियम-क़ायदों में बुरी तरह उलझी हो, उस समाज में नफ़रत के बीज हलके से छींटे पड़ने पर लहलहाने लगते हैं। और इस सबके बीच में जब COVID-19 जैसी जानलेवा महामारी पूरे संसार को घेर लेती है, और उससे लड़ने के लिये दुनिया भर में “सोशल डिस्टैन्सिंग” यानि सामाजिक दूरी बनाने का फॉर्मूला लागू किया जाता है, तब हमें अपनी-अपनी आत्माओं से ईमानदारी से पूछना होगा- क्या हम उन लोगों से दूर रह सकते हैं, जिनका ख़ून-पसीना हमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी पालता-पोसता आया है?
दहशत, नफ़रत और हिकारत में डूबे एक ऐसे समाज में जहां इंसानियत पहले से ही घोर ख़तरे में हो, वहां कोरोना वायरस से जन्मी स्थितियां हम सबके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। वक़्त की ज़रूरत है कि शरीरों के बीच की दूरी बरक़रार रखते हुए और एक दूसरे के जिस्मोजान की पूरी हिफ़ाज़त करते हुए हम इतनी मज़बूती से एक साथ खड़े हों कि एक-दूजे का सबसे ठोस सहारा और हिम्मत बन सकें। अगर एक समाज के रूप हम ऐसा संकल्प लेने से चूकते रहे तो कोरोना की शह में इंसानियत का लॉकडाउन जारी रहेगा और हम इस महामारी से कभी नहीं उबर पाएंगे।
Article by: