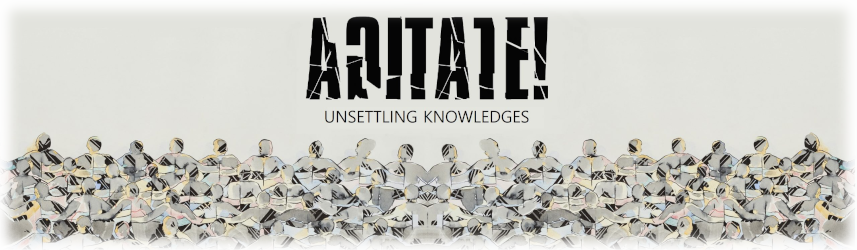Carrying Silences Across Borders: Tarun Kumar Speaks with Abdul Aijaz and Richa Nagar
चुप्पियाँ और सरहदें:
तरुण कुमार के साथ अब्दुल ऐजाज़ और ऋचा नागर की बातचीत
Tarun Kumar, Abdul Aijaz, & Richa Nagar

A scene from Chup, Bombay, 5th August 2023. L to R: Tarun, Sudeepta, Chitra, Manish. Courtesy: Parakh Theatre Archive.
Posters for Chup.
All images courtesy: Parakh Theatre Archive.
ऐजाज़ व ऋचा/ Aijaz & Richa:
तरुण, आप और परख फ़वाद ख़ान द्वारा लिखित नाटक ‘चुप’ तक कैसे पहुँचे? जब आपने इसे पहली बार पढ़ा तो कैसा महसूस हुआ? आपने क्यों और कैसे तय किया कि इस नाटक को उठाना है? आपने चुप की दुनिया को अपने इर्द गिर्द की दुनिया से कैसे जोड़ा?
तरुण/ Tarun:
चुप ऋचा नागर की पाकिस्तान यात्रा की देन है। इनकी फ़वाद ख़ान से कराची में मुलाक़ात हुई और इन दोनों की इस नाटक पर चर्चा हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही ऋचा ने मुझसे इसकी स्क्रिप्ट साझा की और पूछा, “पढ़ कर बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है?” मुझे पहली रीडिंग में हीचुप खामोशियों को तोड़ता हुआ नाटक ज़्यादा लगा, जिसमें कहीं-न-कहीं शोर था। शोर जो अंदर-ही-अंदर रेंगता और कसमसाता है, और कहीं-कहीं चीख़ता भी है। इस शोर को वही समझ सकता है जिसका कोई अपना जीते जी आँखों के सामने से ग़ायब हो चुका हो। वो उस गुमशुदा अपने की ग़ैर-मौजूदगी को कैसे बर्दाश्त करता है? उसको कहाँ-कहाँ ढूंढता है? उसे किस तरह उस ग़ायब शख़्स की मौजूदगी का एहसास हर आहट और सरसराहट में होता है—कहीं कुछ खटकता भर है तो वो इधर-उधर निहारने लगता है।अपने अज़ीज़ को खोजने के लिए न जाने किन-किन गलियों और राहों में भागता है। राह चलते लोगों के चेहरों को आँखें गाड़ कर देखता है कि कहीं ऐसा न हो कि उसके दिल का टुकड़ा किसी अलग भेस में उसके सामने आ जाये और ख़ुदा-न-ख़ास्ता वह अगर उसको पहचान न सका तो बड़ा ज़ुल्म हो जायेगा। इस सब ऊहापोह में एक समय के बाद उसकी ज़िन्दगी थम कर रह जाती है और वह एक तरह की ख़ामोशी ओढ़ लेता है, जो दरअसल उसकी दिमाग़ी थकन होती है। वह ख़ामोशी, जिसे चुप्पी कहते हैं, अरीब-क़रीब के लोगों की दी हुई संज्ञा होती है—चूँकि यह उनका सफ़र नहीं है इसलिए शायद उनके पास उस हाल को बयान करने के लिए और कोई लफ़्ज़ नहीं होता। मगर सही मायनों में उस ख़ामोशी को शब्दों और हरफ़ों में कोई नाम दिया जाये तो वह एक शोर ही है जो अपनों की नीदें उड़ा देता है।
किरदारों की बात की जाये तो सलमान गुमशुदा साद/ ज़ैन का बड़ा भाई है। सलमान की बीवी का इंतक़ाल हो चुका है और वो साद/ ज़ैन की बीवी रबिया के साथ शादी करने के लिए सिर्फ़ बेताब ही नहीं है, बल्कि उसके साथ दुबई में जाकर बसने का इरादा उसके पूरे जिस्मोदिमाग़ में एक अलग ही हलचल मचाये है। परिवार में सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई एक माँ है, जिसकी राजनैतिक पकड़ भी मज़बूत है। और एक ऊंचा सुनने वाला बाप है, जिसे घर और दुनियादारी को समझने का गहरा तजुर्बा है। रबिया, यानी गुमशुदा साद/ ज़ैन की जवान बीवी, घर के हर मख़लूक़ के लिए पूरी शिद्दत से लगी रहती है, और सबकी ख़िदमत करती नज़र आती है। उसके बाप ने साद और सलमान के वालिद और अपने भाई को कभी बड़ा धोखा दिया था, इसलिए अब वह एक और बदनामी के दाग़ को अपने दामन पर क़तई लगने नहीं देना चाहती। सलमान की बिन माँ की एक नौ साल की बच्ची है, ज़ारा, जिसके लिए उसकी चची रबिया ही उसकी ज़िन्दगी है।
शुरू से ही सभी साद के गुम होने को लेकर परेशान हैं। वह साढ़े तीन साल से ग़ायब है। इधर तीन दिनों से अम्मी और सलमान के मोबाइल फ़ोन्स पर मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, और घर में सेल फ़ोन का इस्तेमाल बस यही दोनों करते हैं, हाँलाँकि ज़ारा ज़रूर एक दिन अपनी दादी के फ़ोन पर कुछ बात करती दिखाई देती है। इन रहस्यमयी कॉल्स की वजह से घर में एक महाज़-सा खड़ा हो जाता है। पूरा नाटक कोई दस दिनों के इर्द गिर्द की कहानी है—इस बीच मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनैतिक ऊहापोह, प्रताड़ना, शोषण, और मजबूरियों का इतना मिला-जुला भावनात्मक चक्र खड़ा होता है जिसमें न किसी को ग़लत कहा जा सकता है, न ही किसी को सही। यही इस नाटक की बहुत बड़ी ख़ूबी भी है।
तो अब नाटक के कथानक से मुम्बई की तरफ़ आते हैं।
इधर कई महीनों से मेरे मन में ख़याल आ रहा था कि छोटी कास्ट के नाटकों को तैयार किया जाये, ख़ासकर मुम्बई में, क्योंकि यहाँ कुछ ही दिनों में नए परिंदे थिएटर का दाना छोड़ कर वेब सीरीज़, टेलीविज़न, और फ़िल्मों में अपनी आज़माइश शुरू कर देते हैं। आप उनको रोक भी नहीं सकते क्योंकि सभी अपनी रोज़ी रोटी और फ़िल्मी चकाचौंध के चक्कर में ही अपने घर-बार छोड़ कर यहाँ तक आते हैं। यही हाल प्रशिक्षित कलाकारों का भी है जो ड्रामा स्कूलों और अकादमियों से पास होकर निकलते हैं। इन सभी को सरकारी अनुदान पर, यानी देश के लोगों द्वारा भरे गये इनकम टैक्स की राशि से, पढ़ाया-लिखाया जाता है, उसी तरह जैसे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी और तमाम मेडिकल कॉलेजों में सरकारी अनुदान के सहारे सब्सिडाइज़्ड फ़ीस पर पढ़ाया जाता है। तो एक दौर में इन छात्रों के साथ एक अनुबंध हुआ करता था कि यह पहले देश के गाँवों और क़स्बों में अपनी सेवाएं देंगे, मगर होता ठीक इसका उल्टा है। जैसे, ये सभी पढ़ने-लिखने के बाद विदेशों में नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरह इन नाट्य अकादमियों को भी सरकार एक बड़ा अनुदान देती है ताकि यह छात्र कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपने समाज को समृद्ध करें। मगर अक्सर हम अपने प्रान्तों में लौटकर वापस ही नहीं जाते हैं, न ही रंगमंच को इतनी गंभीरता से लेते हैं, और फ़िल्मों और सीरियल्स में काम करने के लिए दिल्ली और मुम्बई का रुख़ कर लेते हैं। इसमें हमारे देश और दुनिया में पसरे सिस्टम्स का भी ख़ासा योगदान है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है।

ख़ैर, मुम्बई में ये दिक़्क़त हर तरह के रंगकर्मी को झेलनी ही पड़ती है और इसके लिए दूरअंदेशी से काम करना सही रहता है। हर किरदार के लिए कम से कम दो कलाकारों को तैयार करना भी हमारी मज़बूरी बन चुकी है। कब कौन नाराज़ हो जाये या उसको अचानक कोई काम मिल जाये और वो अपने रंगकर्म के ज़बानी अनुबंध को एकदम से नज़रअंदाज़ करके चला जाये। फिर आप चाहे जो कर लें, कैमरे के सामने काम करने की उसकी तमन्ना है तो है। अपनी पहली तरजीह, यानी फ़िल्म, के आगे वो रंगमंच के काम को कभी भी ठुकरा कर जा सकता है, क्योंकि वहाँ उसको काम-चलाऊ पैसा मिल जाता है, और अपने घर और समाज के सामने मुँह उजियारा करने का सौभाग्य भी, कि देखो हमें काम मिल रहा है, और हम कलाकार हैं। ख़ैर, ये सब गहरे और विचारणीय बिंदु हैं जिनके लिए हमें उन हालात पर विचार करना होगा जिनके चलते हमारी अपनी मानसिकता धीरे-धीरे ये सब स्वीकार करती चली गयी है। लेकिन इतना तो साफ़ है कि फ़ुल-टाइम रंगकर्म तो तक़रीबन नाट्य स्कूलों और रेपर्टरी कंपनी के अनुबंधित कलाकारों के साथ ही संभव है।
मैंने चुप पढ़ते ही ऋचा से इस नाटक को खेलने के लिए हामी भर दी। मुझे नाटक को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ग़ायब किये छात्र नजीब अहमद की याद आयी, और नजीब की माँ को देखते हुए मेरे मन में साद/ ज़ैन की माँ और उन तमाम गुमशुदा लोगों की माँओं और परिवारों पर क्या बीतता है, ये सब घूमता चला गया। और चूँकि नजीब वाला मसला ताज़ा था, मुझे लगा कि वो ज़ख़्म शायद आज कल के मुंबईया नौजवानों को भी इस नाटक के साथ जोड़ सकेगा। दुनिया भर में जहाँ-जहाँ दमनकारी घटनाएँ हुई हैं, उन सारी जगहों से सैंकड़ों से लेकर लाखों लोगों के ज़बरन ग़ायब किये जाने की वारदातें सामने आयी हैं। फिर चाहे वे हमारे आज के शासक हों, या हमारे ऊपर पहले राज करने वाले ब्रिटिश, या फिर जहाँ-जहाँ गृहयुद्ध या सैन्यीकृत संघर्ष हुआ है, जैसे, श्रीलंका, नेपाल, साउथ अमेरिका, अपार्थेड के समय का दक्षिण अफ़्रीक़ा, ग्वाटेमाला, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, कम्बोडिया, या फिर फ़िलस्तीन, ये नाटक सभी जगहों से जुड़ता है।
फ़वाद की लेखन शैली ने मुझे बाँधा। दुनिया भर से जुड़ते हुए इस नाटक की कहानी और भावनात्मक परतों को मैंने अपने देश और काल के काफ़ी क़रीब पाया। साथ ही, नाटक की अवधि और भाषा भी मुझे काफ़ी अनुकूल लगे। फ़वाद ने दूर और पास, बाहर और भीतर के मुद्दों को इतने सहज और स्वाभाविक तरीक़े से पिरोया गया है कि शायद किसी धर्मावलम्बी को भी कुछ आपत्तिजनक नहीं लगे। मसलन, इसमें किसी संज्ञा (proper noun) का इस्तेमाल हुआ ही नहीं हैं, सिर्फ़ सर्वनामों (pronouns) से दर्शक सहज ही इसकी गहराइयों तक पहुँच जाते हैं। यह भी लेखक की सफलता का द्योतक है।
परख थिएटर में हम नाटकों का चयन सामाजिक न्याय जैसी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें अपने आस-पास घटती घटनाओं और प्रक्रियाओं से जोड़ते हुए करते हैं। इसी प्रतिबद्धता के चलते कुछ सालों पहले हमने कश्मीर को लेकर अपने कश्मीरी साथियों के साथ एक नाटक करने का काम शुरू किया था, लेकिन देश के हालात देखते हुए हम उस नाटक का प्रदर्शन नहीं कर सके। कहीं-न-कहीं ये बात मुझे कुरेदती रहती थी। इसलिए चुप पहली बार पढ़ते ही मैंने महसूस किया कि इस खेल के ज़रिये हम तमाम तरह के एजेंडों के तहत लापता युवाओं से जुड़े मुद्दों को सामने ला सकते हैं। साथ ही, यह नाटक एक ऐसे गंभीर मसले के बारे में बात करने का मौक़ा दे रहा है जिसके बारे में आसानी से बोला नहीं जा सकता। इस लिहाज़ से देखें तो इस नाटक में फ़वाद का किसी जगह या क़ौम के नाम का उल्लेख न करना मुझे ताक़तवर लगा। क्योंकि इससे नाटक लगातार दर्शकों को दिली और दिमाग़ी वर्ज़िश करने के लिए मजबूर करता है। आप बस बैठकर यह नहीं देखते कि हम आपके सामने क्या ला रहे हैं, बल्कि यह खेल लगातार आपको अपना मन खंगालने के लिए चुनौती देता है। नाटक के अंतिम दृश्य को भी देखें तो अम्मी रबिया को ख़ुला के लिए अनुमति दे देती हैं और उसे और सलमान को ज़ारा के साथ चले जाने और अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए कहती हैं। तभी फ़ोन की घंटी फिर से बजती है और यहीं पर नाटक ख़त्म होता है, बिना हमें यह बताये कि रबिया ख़ुला लेना स्वीकार करती है या नहीं। यानी बड़ी राजनीति के मसले और अंतरंग राजनीति के मसले दोनों हमें सवालों के घेरों में छोड़ देते हैं। जवाबों से ज़्यादा सवाल खड़े करना ही कला का उद्देश्य है ताकि हम अहंकार से भर कर उपदेश न दें बल्कि सच्चाई की हर तह को अपने भीतर महसूस करते हुए उससे लगातार जद्दोजहद करते रहें।
तो कुल मिलकर नाटक दमदार लगा और आज के वक़्त के लिए बहुत माक़ूल। एक बार इसके साथ सफ़र करने की ठान ली, तो फ़वाद साहब से भी ऑनलाइन मुलाक़ातें हुईं। पहली गूगल मीट में हमारे कलाकार साथियों ने फ़वाद से पूछा, “आपने सलमान से क्यों बुलवाया है कि अगर वो वापस आ भी जायेगा तो वो लोग उसको खुला नहीं छोड़ेंगे?” जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत संभव है कि उस परिवेश में साद/ ज़ैन के ऊपर ईश निंदा यानि ब्लासफ़मी का इल्ज़ाम लगा कर उसे जेल में डाल दिया जाता। पाकिस्तान के आर्मी जनरल ज़िआ-उल-हक़ ने प्रजातांत्रिक शासन को ख़त्म करके आर्मी रूल स्थापित कर दिया और उन्हीं के शासन काल में पाकिस्तानी हुकूमत एक दूसरे दौर में प्रवेश कर गयी, जिसमें ईश निन्दा को वहाँ सबसे बड़ा गुनाह माना जाने लगा। हिंदुस्तान में मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली भी उसी दिशा में नीतियाँ बना रही है, हमारी सरकार भी अपनी किसी भी तरह की आलोचना करने वाले को बर्दाश्त नहीं करती है और वह जब चाहे तब किसी को भी देशद्रोही या राष्ट्रविरोधी घोषित करने लगी है।
साथियों के साथ चुप में उतरते हुए इस तरह की तमाम चर्चायें चलीं। साथी कलाकार यह समझने के लिए उत्साहित थे कि आख़िर यह मनोवृत्ति कहाँ से आती है कि हम इंसानियत को बाला-ए-ताक़ रख कर सिर्फ़ किसी की सर्वोच्च सत्ता को क़ायम रखना चाहते हैं? वह भी ऐसी सत्ता जो सम्पूर्ण विश्व को बाज़ार—ख़ासतौर से हथियारों के बाज़ार—की नज़र से देखने पर आमादा हो, और जिसके लिए धर्मान्धता को केंद्रित करने से बेहतर दूसरा कोई खेल या तंत्र हो ही नहीं।
सच कहूँ तो चुप नाटक से पहले मौजूदा माहौल में हम लोग इस तरह का कठिन सामूहिक सफ़र कर ही नहीं पाये थे। यहाँ यह भी कह दूँ कि हमारे कलाकार साथी कोई गहरी राजनैतिक सोच वाले नहीं थे। यानी, हम सभी हल्की-फुल्की राजनैतिक समझ रखने वाले लोग थे, जितना किसी भी आम इंसान को समाज में रहने और बातचीत करने भर के लिए थोड़ा-थोड़ा सभी कुछ पता रहता है ताकि कहीं भी बैठकर अपनी छोटी-मोटी प्रतिक्रिया दे सके। भारत की आंतरिक और वैश्विक राजनीति के पहलू इससे ज़्यादा बस हमारे यहाँ के समाचार चैनल्स और व्हाट्सप्प यूनिवर्सिटी ही कवर करते हैं, उनमें भी इतनी ज़्यादा चिल्ल-पों मची रहती है और वैकल्पिक सचों और आवाज़ों को इस क़दर दबाया जाता है कि समाचार अब अपनी उपयोगिता ख़त्म कर के बस एक शोर बन चुके हैं। सी. एन. एन. जैसी कुछ सुप्रसिद्ध विदेशी एजेंसियों की तरह भारत की भी ज़्यादातर समाचार एजेंसियां और मैगज़ीन्स किसी-न-किसी राजनैतिक अजेंडे के तहत ही काम करती हैं। ये एजेंसियां सरकारों की चुनावी छवि सुधारने के लिए और विरोधी पक्ष की मुख़ालफ़त का माहौल बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाती हैं।आज भारत का समाज राजनैतिक विचारधारा के आधार पर बँटने भी लगा है और हालात इतने नाज़ुक हो चुके हैं कि मीडिया से पैदा की जाने वाली दुश्मनियों का असर घर-घर में और क़रीबी संबंधों पर भी दिखाई देने लगा है। ‘जात-पांत के झगड़े छोड़ो, भारत जोड़ो-भारत जोड़ो’ जैसा नारा तो है मगर जोड़ना कौन चाहता है? प्रजातंत्र के नाम पर यहाँ राजशाही और सामंतवाद ही रहा है, प्रजातंत्र बस एक मुग़ालता है। हर किसी को अपनी-अपनी जाति, पंथ, और धर्म का झंडा फहराना है और अपना-अपना गाना ही गाना है। हमारे यहाँ की राजनीति इतनी जागरूक और लुभावनी भी नहीं है, वजह यह कि यहाँ शिक्षित होते ही सामन्ती कीड़ा काम करना शुरू कर देता है—इसलिए शिक्षित वर्ग से ख़ामख़ाँ किसी बड़प्पन की उम्मीद करना ही महा की मूर्खता है। वैश्विक राजनीति भी इससे परे नहीं है कि उस पर गर्व किया जा सके। सभी ने अपनी जनता में भेद-भाव, नस्लवाद, धर्म वग़ैरह के आधार पर, और राष्ट्रीयता का झूठा और खोखला भय दिखा कर, अपनी सत्ता को बढ़ाने और चमकाने का ही काम किया है। प्रजातंत्र के नाम पर अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने की युक्तियाँ चलाते हुए अंधभक्तों जैसी जनता जनार्दन को तैयार किया है। मुख़्तसर में इतना ही, कि आज के हालात समझने के लिए हमें किसी ख़ास घटना या समुदाय की बारीकियों को नहीं, बल्कि तमाम स्तिथियों के इतिहास, भूगोल, और सत्ता-ताक़त के खेलों को बारीकी से समझना होगा। हमें हमारे देश, और हमारे जैसे तमाम देशों, को पिछड़े घोषित किये जाने की गणित को भी समझना होगा। मैं पश्चिमी देशों की उपलब्धियों को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन असमानताओं और युद्धों के बढ़ते दौर में उन्हें ग़ैरबराबरियों और हमारी दुनिया में चल रही अकथनीय हिंसाओं के जनक के रूप मे ज़रूर देखता हूँ। हमारे देशों के नौजवान इन साम्राज्यवादी देशों की शिक्षा और जीवन प्रणाली को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर चलते हैं। बाज़ारीकरण के खेल में फ़्री कंबल, फ़्री इंटरनेट, मंदिर-मस्जिद, और किसी बड़े नेता से मिलती-जुलती शक्लो सूरत वाले को अपना भगवान् मानकर पूजने वाली मानसिकता में ही सिमटा हुआ समाज अपने मतदान का उपयोग करके इस देश के प्रजातंत्र की रक्षा भला कैसे करेगा? जनता जनार्दन ने अपना विवेक और ज़मीर दोनों ही गिरवी रख दिये हैं। और चुप ने हमें इन तमाम तहों और बारीकियों में जाने का एक ज़बरदस्त मौक़ा दिया।

Courtesy: Parakh Theatre Archive.
ऐजाज़ व ऋचा/ Aijaz & Richa:
इस नाटक को आपकी नज़रों से समझना चाहते हैं। आपने इस नाटक को स्क्रिप्ट से स्टेज तक ले जाते हुए कैसा सफ़र किया? इसे समझने की क्या प्रक्रिया थी? आपने इस कहानी को इतने प्यार से निभाया है, इसके पीछे क्या कमिटमेंट था? क्या चीज़ थी जिस ने आप को कहानी के साथ इस क़दर जोड़ दिया?
तरुण/ Tarun:
जैसा मैंने पहले कहा, चुप पूरी ख़ामोशी से चीख़ता है, और बिना किसी को सीधे-सीधे कटघरे में खड़ा किये हुए है कि ये ग़लत है, या ये सही। यह बड़ी ही नज़ाकत और subtlety से हमें ले जाता है उस माहौल में जिसमें इसके किरदार जीते हैं, और हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि यह माहौल कितना अपना है और कितना पराया, और हमारी सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ और मॉरल्स ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाएं भी, कहाँ जाकर टिकते हैं? उस माहौल में क्या मुनासिब है? हमारी ही चाहों के लिए हमारी परिस्थितियां कितनी माक़ूल हैं? यानी चुप एक गहरे मानवीय दृष्टिकोण के साथ हमें चीज़ों को बड़ी पारदर्शिता से देखने और समझने के लिए कहता है और इसीलिए मैं पहली ही रीडिंग में इससे गहराई से जुड़ने लगा।
मुझे और मेरी कास्ट को किरदार तो अपने इर्द गिर्द के ही लगे लेकिन हमारे लिए यह ज़रूरी था कि हम इन किरदारों को किसी ख़ास मज़हबी नज़रिये से देखने के ट्रैप में न आ जाएँ—उस ट्रैप से किसी भी क़ीमत पर बचने की ज़रूरत थी। राइटर ने जिस तरह की लाइन्स किरदारों को दी हैं उनको ज़ेहन में रखकर उनके साथ ईमानदार सफ़र करना था। दृश्यबंद में किसी भी ख़ास तरह के पहनावे के बारे में कोई लाइन नहीं थी सिवाय पहले दृश्य में जब रबिया दाख़िल होती है और नाटककार लिखता है कि उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ है। अब ये बात कोई भी हलके में ले सकता है—आख़िर कोई रात में पानी पीने के लिए उठेगा तो भला क्यों दुपट्टा लेगा? लेकिन यहाँ इस परिवार के रिश्तों की इमारत के बारे में लेखक ने एक ताकीद दी है, जिसे नज़रअंदाज़ करने से रबिया और सलमान के दरम्यान की नाज़ुक कड़ी को समझने में चूक हो जाती। इस नाटक की ग्रेविटी को पूरी इज़्ज़त देते हुए हम सभी कलाकारों ने इसी तरह के तमाम बिंदुओं पर काम करना शुरू किया। सभी लोग सलमान और साद/ ज़ैन के दरम्यान छुपे प्यार, तनाव, मतभेद, और संघर्ष को एक ज़िम्मेदारी के साथ—और अपने सबसे अज़ीज़ और नज़दीकी रिश्तों और पलों में तलाशते हुए—अपने-अपने किरदारों को समझने और सँवारने में लग गए।

हमारे साथियों को जब इस मुद्दे से रूबरू होना पड़ा तो उनके सामने बार-बार कश्मीर घूमता । कश्मीर में काफ़ी तादाद में नौजवानों के ग़ायब किये जाने का सिलसिला आज़ादी और बँटवारे के पहले से ही चल रहा है। इसलिए इस नाटक में उठाये गए मसलों को वहाँ से जोड़ कर देखने पर हम सभी को चीज़ें समझने में सहूलियत हुई। जो समाचारों पत्रों में पढ़ने-सुनने को मिलता रहा था उससे अलग हटकर इस मुद्दे की परत-दर-परत को महसूस करते हुए इस समस्या के मूल को समझने का, और अपने-अपने शरीर, मन, और दिमाग़ से जद्दोजहद करने की एक सच्ची कोशिश करने का मौक़ा मिला।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही देश के विभाजन से उपजे हैं। इस ज़मीन पर धर्म जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दे के आधार पर किया गया बँटवारा, यानी ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दिया सबसे भयंकर सदमा, दरअसल हमारा नकबा था, जिसके असरात आज तक हम रोज़ जी रहे हैं। राजनैतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में मानव जाति पर किया गया कितना बड़ा और घटिया प्रयोग जिसके तहत कितना बड़ा नर संहार हुआ, जिसकी कल्पना करते ही पूरे समाज की रूह काँप उठती है! विस्थापन का इतना बड़ा फ़ैसला ब्रिटिश साम्राज्य ने सिर्फ़, और सिर्फ़, अपनी औपनिवेशिक ताक़त को भविष्य में भी क़ायम रखने के लिए किया, और एक फली-फूली मानवीय सभ्यता को नष्ट करने के साथ-साथ वे हम सबको एक लम्बे समय के लिए धार्मिक सम्प्रदायिकता के अंधे कुंए में फेंक गए। ब्रिटिश शासक भारत का भरपूर उपभोग करने के बाद इस बँटे हुए देश को चुनिंदा सवर्णों और विदेशों में पढ़े-लिखे गिने चुने लोगों के हवाले करके चलते बने। इस कूटनीति के चलते हम आज भी बुरी तरह से हिन्दू-मुस्लिम में बँटे और भटके हुए हैं।
चुप नाटक में मौजूद तमाम तहों और घटना क्रम को समझने के लिए विभाजन के बारे में सोचना हमें बहुत ही ज़रूरी लगा। यानी हम आज इस मक़ाम पर कैसे और क्यों खड़े हुए हैं? कैसे हमारी सरकारों ने अपनी-अपनी सत्ता को चमकाये रखने के लिए भयंकर मुफ़लिसी, बेरोज़गारी, और अशिक्षा बनाये रखी और साथ-साथ ध्रुवीकरण के दौर में धार्मिक राष्ट्रवाद और उग्रवाद के ज़रिये नफ़रत, असहिष्णुता, और हिंसा को बढ़ावा देते रहे, जिसके बीज पहले ही तकसीम के रूप में पल्लवित हो चुके थे। मैं यह सोचकर हैरत में पड़ जाता हूँ कि इतने बड़े भौगोलिक भू-खंड में—जहाँ इतनी भाषाएँ, आचार-विचार, और रहन-सहन हों, जहाँ एक तरफ़ नदियों का जाल हो, दूसरी तरफ़ पर्वत श्रृंखलायें हों, और तीसरी और चौथी ओर अरब सागर और हिंद महासागर हों—ऐसे में रेडक्लिफ नाम का कोई शख़्स पहली बार भारत आता है, और कुल जमा पाँच हफ़्तों में हमारे भौगोलिक, सांस्कृतिक, जनसांख्यिक, व भाषायी भेदों और गहराईयों को दर किनार करते हुए, और ख़ालिस राजनीति से प्रेरित और पूर्व निर्धारित सोची समझी चाल के तहत, निहायत संवेदनहीनता के साथ काग़ज़ पर लकीरें खींच कर मौक़ा परस्त नेताओं की अंधी सहमति के आधार पर हमें काट कर चला जाता है।
भारत का विभाजन दोनों तरफ़ के बहुतायत लोगों को स्वीकार नहीं था और आम जनता को तो कोई भान तक नहीं था। ये कृत्य भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बिलकुल अमानवीय होने के साथ-साथ एक दुर्दांत काम था। विभाजन की रेखाओं के आर-पार किसी को ख़बर ही नहीं थी कि उनको कब किसने और क्यों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बना दिया था। उनको जाना कहाँ था और कहाँ नहीं, कुछ खबर ही नहीं थी। प्रतिक्रिया स्वरुप, अवाम के दिलों में एक अजब सी ख़ामोशी तारी थी। उसके बाद जो ख़ून-ख़राबा, बलात्कार, चोरी-डकैती हुई वो विस्थापन और इंसानियत के लुट जाने का वीभत्स पन्ना है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित ‘तमस’ काफ़ी हद तक इस पन्ने को पढ़ने में सफल होता है, लेकिन दिलो-दिमाग़ की विक्षिप्तता को जिस तरह सआदत हसन मंटो ने अपनी कहानियों की मार्फ़त, ख़ास कर “टोबा टेक सिंह” में, दर्शाया है उस तरह और किसी ने नहीं वैसे तकसीम को समझना किसी कहानी या उपन्यास के पढ़ लेने भर का काम नहीं है। “टोबा टेक सिंह” में जिस मानसिक स्थिति को उकेरा गया है वो क्या है, इसको महसूस करने, और करते रहने, की बेहद ज़रूरत है।
हमारी बँटी हुई आज़ादी का झुनझुना कुछ लोगों को बड़ा ख़ूबसूरत दिख रहा था, और दोनों पक्षों के कुछ नेताओं में उसको थामने के अजीब से उतावलेपन का भरपूर फ़ायदा उठा कर ब्रिटिश शासकों ने इस देश के ताने बाने को छिन्न-भिन्न्न कर दिया, और हम आज तक इसका ज़हर पी रहे हैं। आज हमारी मौजूदा पीढ़ियां तक इसका शिकार बनायीं जा रही हैं—उस पार और इस पार दोनों देशों का एक ही सच है। उन्हीं दुष्परिणामों की एक मिसाल ये नाटक चुप है।
अब तकसीम से आज़ाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दौर में आयें तो मानवाधिकार के लिए बनी संस्थाओं का पहले तो कोई नामोनिशान भी नहीं था। ज़बरन ग़ायब किए जाने की घटनाओं को सबसे पहले एक प्रमुख मानवाधिकार समस्या के रूप में पहचाना गया था 1970 के दशक में, जब चिली में मानवाधिकार वकीलों ने देखा कि जिन क़ैदियों के वे केस देख रहे थे वो क़ैदी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे, भले ही ज़ाहिरा तौर पर चिली के सुरक्षा बलों द्वारा उनको किसी न किसी बहाने से हिरासत में रखा जाना जारी रहा।
चुप को करते हुए मुझे एक वाक़या याद आया जो मैंने अपने साथी कलाकारों के साथ भी साझा किया। बात फरवरी १९९० की है। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के प्रख्यात फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल साहब के एक सहायक निर्देशक थे, मनदीप कक्कड़। बैंगलोर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते समय गोल्फ़ कोर्स के ऊपर उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मनदीप जी की बॉडी नहीं मिली थी, बस जहाज़ के मलबे से कुछ दूरी पर उनका परिचय कार्ड मिला था। उनकी बीवी के लिए और परिवार के लिए यह समझना मुश्किल था कि उनका हुआ क्या, क्योंकि अपने का न होना एक ऐसी चीज़ है कि आँखें जब तक देखती नहीं, तब तक दिमाग़ को यक़ीन दिलाना मुश्किल हो जाता है। उनकी पत्नी को दिन भर और रात बिरात जब भी कोई आहट होती तो यही लगता कि शायद वो आ गये हैं। नाटक में फ़वाद ख़ान ने पापा के ज़हन में वैसा ही खटका दर्शाया है। जिस इंसान को हियरिंग ऐड के बग़ैर सुनाई नहीं देता है उसको हर वक़्त दरवाज़े पर किसी के खटखटाने की सुगबुगाहट होती रहती है, जो कि एक गहरी दिमाग़ी चोट और सदमे को नुमाइंदा करती है। नाटक में माँ का संघर्ष एक अलग स्तर पर है और पापा का अलग। इसी तरह रबिया, सलमान, और ज़ारा सभी के दर्द एक-से होते हुए भी मुख़्तलिफ़ शक्लों में दिखाई देते हैं। मसलन, ज़ारा फ़ोन पर बात करने का अगर अभिनय भी करती है तो उसकी बातचीत में भी उसी दर्द की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अपने चचा के ग़ायब होने का और उससे जुड़े घटना क्रमों का उसके ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ रहा है, परोक्ष-अपरोक्ष रूप में, जिसका ज़िक्र सलमान रबिया से भी करता है।
तो इन बेहद नाज़ुक और आत्मीय मानसिक स्थितियों को कैसे पिरोएं गुमशुदगी के उस लम्बे इतिहास में जिससे हिंदुस्तान के तमाम सीमावर्ती इलाक़े वाबस्ता हैं। आँकड़े पेश करने चलेंगे तो यह बात बहुत खिंच जायेगी। मुख़्तसर में इतना ही कि एक बार फ़वाद ख़ान के चुप नाटक को उठा लिया, फिर इसकी गहराईयों में उतरने के लिए ख़ासी मशक़्क़त की। इस बीच मेरी ऋचा से लगातार बातचीत तो चल ही रही थी, साथ ही साथ ऋचा कलाकारों के साथ भी ऑनलाइन ज़ूम पर मिलकर इस नाटक से जुड़ी परतों पर काफ़ी रौशनी डालती रहीं। पहले कोरोना काल में हमारे कई ऑनलाइन ऑडियो शो हुए और उनके दौरान चर्चाएं चली, और अब २०२२ से स्टेज शो चल रहे हैं और चर्चाएं जारी हैं। किसी भी नाटक के साथ इतना लम्बा चलने का मेरा यह पहला अनुभव है। कहीं-न-कहीं चुप एक गहरे दर्द का हिस्सा बन गया है जिसकी टीसें ख़त्म ही नहीं हो रहीं। चूँकि चुप बहुतेरे मानवीय पहलुओं को छूता है इसलिए इसका दर्द शायद हमेशा हरा ही रहेगा क्योंकि ग़ायब किए जाने के ज़ख्म कहीं-न-कहीं मौत के ज़ख़्म से भी ज़्यादा तकलीफ़देह हैं। यह मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ी लानत है जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ।

ऐजाज़ व ऋचा/ Aijaz & Richa:
जब आपने नाटक उठाया तभी दुनिया के दरवाज़े पर कोविड-19 ने दस्तक दी। इस नाटक को साकार करने के सफ़र में परख को कैसी दुश्वारियाँ और चुनौतियाँ झेलनी पड़ीं ?
तरुण/ Tarun:
हम लोगों की पहली मीटिंग उन्तीस फ़रवरी २०२० को मेरे घर से शुरू हुई थी। हम रोज़ शाम चार बजे रीडिंग करने लगे। काफ़ी कलाकारों को बुलाया, सभी उत्साहित थे कि कुछ नया हो रहा है। अभी हमारे रीडिंग सत्र शुरू ही हुए थे कि अठ्ठारह मार्च से कोरोना की वजह से लॉकडाउन की ख़बरें आनी शुरू हुईं, फिर इक्कीस मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन घोषित किया और उसके बाद सभी कुछ थम सा गया।
अब बिना इसमें जाए कि यह लॉकडाउन कैसे क्रियान्वित हुआ और इसने हमें अपने ही देश और दुनिया के क्या-क्या नए रंग दिखाये, मैं नाटक पर ही आता हूँ। मार्च २०२० के बाद के महीनों में—और ईमानदारी से देखें तो लगभग दो साल तक—पूरा विश्व एक अजीब से सदमे के दौर से गुज़रा। सभी तरफ़ एक अजब चुप्पी, और दिमाग़ को सुन्न करने वाला एक लम्बा सन्नाटा पसरा हुआ था। क्या बूढ़े, क्या जवान, और क्या बच्चे, ये मौत जैसी ख़ामोशी हम सभी को डराकर और भी चुप करा रही थी, जिसके लिए हमारे दिलोदिमाग़ तैयार नहीं थे। हम लोग कुछ दिनों तक तो रिहर्सल कर ही नहीं सके। कुछ कलाकारों के घर वालों ने कुल लॉकडाउन लगने से पहले समय रहते अपने बच्चों पर दबाव बनाया कि वे घर वापस आ जायें, लेकिन जो कलाकार नहीं जा सके वे भी इस बंद के पहले एक लम्बे समय के लिये अपने-अपने घरों में खाना-पीना-राशन जुटाने में लगे थे। सारे इंतज़ाम करते हुए धीरे-धीरे हम सभी इस बंद के लिए दिमाग़ी रूप से तैयार हो रहे थे। जाति-वर्ग के ताने-बाने में हम कलाकारों की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि हमारी वह दशा नहीं हुई जो इस देश के तमाम प्रवासी मज़दूरों की हुई।
इस बीच हम लोगों की आपस में एक दूसरे के हाल लेने के लिये बातचीत चलती रही। फिर हमने जल्द ही ज़ूम और गूगल मीट पर मिलने का फ़ैसला किया और रिहर्सल शुरू कर दी। पहले-पहल ये ऑनलाइन रिहर्सल का काम ख़ासी चुनौतियों से भरा लगा। जिस काम को अब तक हम लोग रूबरू करने के आदी थे, वही काम अब हम अपने-अपने माँ-बाप या रिश्तेदारों के घरों और शहरों में बैठ कर कर रहे थे। सभी कलाकारों के समर्पण भाव को देखते हुए और बहुत-सी पेचीदगियों को सोच समझकर ही काम चल रहा था। मगर खेल को ज़्यादा रिफ़ाइन करने का काम यही सोचकर नहीं किया जा रहा था कि पता नहीं कलाकारों के घरों में क्या चल रहा है? वो कहीं किसी तरह के मानसिक और आर्थिक तनाव या दबाव में तो नहीं है या कुछ ऐसा भी हो सकता है जो वो साझा नहीं कर पा रहे हों। हम सभी लोगों की समस्याएं तक़रीबन एक जैसी ही थीं। पहले हम में से ज़्यादातर लोगों के घरों में काम करने के लिए हेल्पर्स आते थे, किसी के यहाँ पूरे दिन के लिए और किसी-किसी के यहाँ ख़ाली खाना बनाने या साफ़ सफ़ाई के लिए। मगर लॉकडाउन के बाद तमाम कामगार साथी ऐसे डरावने माहौल में थे जहाँ वो किसी के आसरे नहीं रह सकते थे, और वे बेहद कठिन सफ़र तय करके अपने-अपने घर वापस चले गए थे। तो इन तमाम वजहों से सभी कलाकारों के ऊपर घरेलू काम काज का अतिरिक्त कार्यभार था, और इन सब हालात का लिहाज़ करते हुए ही रिहर्सल का काम चल रहा था।
मगर मुझे ये रंगमंच के साथ और कलाकारों के साथ नाइंसाफी जैसा भी लग रहा था, और यह भी कि जब हम लोग फ़्लोर पर मिलेंगे तब सब कुछ एकदम मुख़्तलिफ़ होगा और यह शायद ज़्यादती होगी कलाकारों और उनकी मेहनत के साथ। एक अच्छी ख़ासी शुरूआत के बाद यही सब सोच कर कुछ दिनों के लिए रिहर्सल को फिर रोक दिया।
सच कहूँ तो रिहर्सल को रोकने की एक वजह कोरोना वायरस भी था क्योंकि हम सभी अपने घरों के बाहर और भीतर के माहौल से भयभीत थे। तमाम क़रीबी दोस्तों और अज़ीज़ों की मौतें तो हो ही रही थीं, साथ ही बंद के दौरान सरकार ने सभी यातायात बंद कर दिये थे जिसके बाद तमाम प्रवासी मज़दूरों और श्रमिकों के धैर्य का बाँध टूटना लाज़मी था। ये सभी बंद के दौरान छोटे-छोटे कमरों में एक तरह से क़ैदियों की तरह रह रहे थे। मुम्बई का धारावी एशिया का सबसे बड़ा इनफ़ॉर्मल सेट्लमेंट माना जाता है, वहाँ झुग्गी-झोपड़ियों में तमाम कामगार सुबह-शाम की अलग-अलग शिफ़्टस में काम करते थे, तो अदला-बदली में उतनी ही जगह में उन सबकी गुज़र-बसर हो जाती थी। मगर अब बंद के दौरान तो सभी को उतनी ही जगह में चौबीसों घंटे रहना था, वो भी एक-दो दिन के लिए नहीं, बल्कि लगातार। मार्च से मई २०२० तक का वक़्त उन्होंने कैसे जीया ये वही जानते हैं, लेकिन फिर उनका संयम जवाब दे गया क्योंकि काम-काज न होने की वजह से लोग किराया नहीं दे पा रहे थे और खाने पीने की दिक़्क़तें तो थीं ही। ऊपर से इर्द-गिर्द घटती मौतें और उनके अंतिम क्रिया-कर्म की ख़बरों को जिस तरह सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था, उसको देख सुनकर किसी का भी दिल दहल जाये। सरकार से सबका भरोसा उठ गया था। इसलिए सब अपने-अपने ठिकानों से बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन की तरफ़ निकल पड़े। वहाँ पहुँचने पर उन्हें जब पता चला कि उनके लिए बसें और ट्रेनें तो हैं ही नहीं, ऐसे में उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचा और वे लोग अपने सामान अपने ऊपर लाद कर जैसे-तैसे अपने मूल गाँवों की तरफ़ पैदल ही चल पड़े। ये मज़दूर भूखे, नंगे पाँव, अपने छोटे-छोटे बच्चों को कांधों पर लिए, दम तोड़ते चले तो जा रहे थे, मगर यहाँ एक और ज़ुल्म खड़ा हो गया, क्योंकि सरकार की सख़्त मनादी थी और पुलिस का बेरहम पहरा था। उनसे बचने के लिए ये लोग छुपते-छुपाते अंदरूनी रास्तों का सहारा लेते हुए चलने को मजबूर हुए। यात्री रेलें तो चल नहीं रही थीं, बस थोड़ी-बहुत गुड्स ट्रेनें चल रही थीं, और इसी धोखे और मजबूरी में जब कुछ मज़दूरों ने पटरियों के किनारे-किनारे चलने का रास्ता चुना तो वहाँ भी मौत मुँह फैलाये बैठी थी। ये लोग थक कर, और इस ख़याल में कि ट्रेनें तो चल नहीं रही हैं, वहीं रेलवे ट्रैक्स पर सो गए। कई सौ मील पैदल चलने के बाद ऐसी थकन का तारी होना लाज़मी था। ऐसे में उनको एक माल गाड़ी कुचल कर चली गयी।

आपके सवालों के जवाब देते हुए ये सब याद करना ज़रूरी लग रहा है क्योंकि इन दिल दहला देने वाली घटनाओं के साथ ही हम चुप के साथ अपना शुरूआती सफ़र कर रहे थे। सरकार के ख़िलाफ़ देशभर में ख़ासा रोष था, कि उन्होंने जल्दबाज़ी में लॉकडाउन क्यों लगा दिया, जबकि लॉकडाउन से पहले डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा का बहुत बड़ा जश्न मनाया गया था, और मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन का कार्यक्रम भी चल रहा था। उसके तुरंत बाद बंद की घोषणा कैसे और क्यों की गयी, देश की जनता इसका हिसाब माँग रही थी, मगर सरकार चुप थी। हमारे तमाम मज़दूर साथी भी शहरों में फंसे हुए थे और हम उनके सहयोग के लिए भी काम कर रहे थे। सभी लोग एक तरह के मानसिक और आर्थिक तंगी के दर्दनाक और बेरहम माहौल से गुज़र रहे थे। भविष्य अंधकारमय दिख रहा था।
ऐसी दहशत, मौत, और चुप्पियों के दौर में ही मई में बंद हुई रिहर्सल को हमने तिबारा शुरू किया २० जून को। ऋचा के साथ लगातार प्लानिंग और चर्चाएं हो रही थीं। सोच समझकर तय हुआ कि हम सिर्फ़ रिहर्सल तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इस नाटक का ऑनलाइन प्रदर्शन भी ज़रूर करेंगे। इस निर्णय से सारे कलाकार साथियों का उत्साह बढ़ गया और हम लोग रोज़ चार घंटे ऑनलाइन मिलने लगे।
कोरोना काल के बंद के दौरान हुए अनुभवों के चलते हम कश्मीर के लोगों से भी अलग ढंग से जुड़ सके। हमने पहली बार उनकी रोज़ मर्राह की ज़िन्दगी को महसूस करने की कोशिश की। कश्मीर में साल-दर-साल आये दिन जब कर्फ़्यू और बंद लगते हैं तो वहाँ के लोगों को कैसा महसूस होता होगा। हाँलाँकि इस बंद का उस बंद से कोई सरोकार नहीं है और ना ही कोई मुक़ाबला। दोनों के मनोवैज्ञानिक दबाव और प्रभाव बहुत अलहदा हैं। कोरोना के बंद में एक क़ातिल बीमारी से संक्रमित होने और उससे मरने के डर ने एक अजब तांडव मचाया हुआ था। जिनको घर बैठ कर काम करने या रहने की आदत नहीं थी, या जिनके अपने लोग दूसरे शहरों और देशों में रह रहे थे या फंस गए थे उन सभी को अपनों की कितनी फ़िक्र थी ये वीडियो कॉल्स में उनके चेहरों और बातों में साफ़ देखी जा सकती थी। लेकिन फिर भी, हम लोगों के पास अपने फ़ोन्स थे, इंटरनेट की सुविधा थी, कईयों के लिए खाने-पीने की डिलिवरी भी ऑनलाइन आर्डर दे कर हो ही रही थी। फिर भी इन हालात ने हमें गुमशुदा किये गए लोगों के परिवेशों से एक अलग गहराई और ईमानदारी से जुड़ने के लिए झकझोरा। हम अलग ढंग से महसूस कर पाए कि किसी अवाम को अगर पैंतीस साल या सत्तर साल लगातार एक सिस्टम के तहत, चाहे इस पार हो या उस पार, भयंकर दुविधाओं, दबावों, डरों, और मुसीबतों से गुज़रने के लिए मजबूर कर दिया जाये तो उन के दिलो-दिमाग़ पर क्या गुज़रती होगी? जहाँ फ़ोन लाइन्स और इंटरनेट बंद कर दिए जाएँ, पढ़ाई-नौकरी-कारोबार और रोज़मर्राह की चीज़ें सब बर्बाद हो जाएँ, और कोई किसी से बात भी नहीं कर सके, कहीं आ-जा नहीं सके, ठीक से खा-पी नहीं सके, तो ऐसी जगह भला क्या अंजाम होगा? ऐसे में जब वहाँ के लोग अपने ही वतन में दर बदर हो जाएँ, और शासक यह उम्मीद करें कि वो सारे के सारे सरपरस्त और ख़ामोश हो जाएँ, और फिर देश की बाक़ी अवाम और मीडिया भी इस पूरे कृत्य पर आँख मूँद कर मूक दर्शक ही नहीं बल्कि साथी बन जाये। और ऐसे में इस सबके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले न जाने कितने जवान लोग गुमशुदा कर दिए जाएँ और न जाने कितनों को अपने से जुदा कर दिया जाये, तब क्या गुज़रती होगी उस संसार में?
कलाकार साथी यह सारे मंज़र अपने शरीर में उतारते हुए गुमशुदगी के क़िस्से खंगालते गए। मैंने १९९० के दौर के बारे में भी सोचा। उस समय, जब मैं अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी के कनवोकेशन में शामिल होने के लिए गया था, तमाम कश्मीरी शरणार्थी सड़कों पर टेंट लगाकर खुले में जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे। उस समय का मीडिया, जो सरकारी दूरदर्शन और समाचार पत्रों तक ही सीमित था, खुल कर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था। आज का वक़्त होता तो शायद दुनिया भर की तमाम संस्थाएं और संगठन ट्विटर और फ़ेसबुक पर लिखते-पढ़ते और उस वक़्त की मौजूदा सरकार से गुहार लगाते, और शायद दुनिया भर के एक्टिविस्ट और मानवाधिकार समितियाँ पेटीशन दायर करतीं। लेकिन जैसा कि हम आज अपने देशों और अभी ग़ज़ा में मचे क़त्लेआम में देख रहे हैं, खुल कर सच बोलने वाले मीडिया और लोगों के मुँह बंद करना भी एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया है।
मैं ये सब कहते हुए उन हालात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके तहत एक इंसान को अपना घर छोड़ने जैसी मजबूरी इख़्तियार करनी पड़ जाती है या फिर उसको उठा कर ग़ायब कर दिया जाता है। और फिर उसके पीछे पूरा एक घर ही नहीं, बल्कि उसके तमाम दोस्त और उसे जानने वाले भी हमेशा परेशान रहते हैं। राजनैतिक और सामाजिक पहलुओं के साथ-साथ मैं उन तमाम तंज़ीमों की तरफ़ भी आपको ग़ौर करने के लिए छोड़ रहा हूँ, जिनकी तरफ़ लेखक ने इशारा किया है। चुप में सलमान कहता है कि अगर साद/ ज़ैन वापस आ भी गया, तो भी “वो” उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, बल्कि उसको किसी न किसी केस में उलझा कर जेल में डाल देंगे। इस जुमले के सहारे लेखक सिस्टम की ख़तरनाक क़ानूनी चालों की बात कर रहा है। यानी, जो सिस्टम में हैं वे उस गुमशुदा को, ‘उस’ दुनिया की और ‘उसके’ पीछे छिपी हुयी सच्चाई साझा और उसका खुलासा करने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। ये बात बिलकुल वैसी ही है जैसी हम मुम्बइया फिल्मों में सुनते हैं, जब अंडर वर्ल्ड डॉन अपने किसी सदस्य को गैंग जॉइन करते वक़्त समझाता है कि सोच लो यहाँ आने का रास्ता तो है लेकिन यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है।
यह बात सुनने में अजीब लग सकती है लेकिन कोरोना के माहौल को हम सभी एक तरह की गुमशुदगी से जोड़ कर भी देख रहे थे, क्योंकि जिसको भी कोरोना होता, उसको घरवालों से दूर ले जाया जा रहा था और मरीज़ की ट्रैकिंग का हिसाब-किताब बहुत लचर था। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि उनके मरीज़ की कैसी हालत है और अमूमन घर वालों को अचानक उसके मरने की ख़बर ही मिलती थी, या कभी-कभी तो वो भी नहीं मिल रही थी। मृत शरीर भी परिवार वालों को नहीं दिए जा रहे थे, बस मुर्दे को एक काली पॉलिथीन में लपेट कर और किसी एकांत जगह पर ले जाकर उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती, वो भी सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में। परिवार वाले और मरीज़ ही नहीं बल्कि पूरा समाज इसी सबसे जने सदमे और डर में जी रहा था। तो कलाकारों ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि कैसा लगता होगा जब आपको अपना कोई प्रियजन अन्येष्टि के लिए भी देखने को न मिले? जब उसको उसके अपनों ने अपनी आँखों के सामने मरता न देखकर सिर्फ़ एक काली पॉलिथीन में तमाम लाशों के बीच लेटा देखा हो? ऐसी दहशत और ग़म से कोई इंसान कभी निकल भी पाता है? लोग आपस में तुक्के भी लगाते कि मरने के बाद भला किसी मुर्दे में रहा वायरस किसी ज़िंदा इंसान को कैसे संक्रमित कर सकता है, लेकिन सिस्टम पर यक़ीन करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। कौन जाने कि ये भयावह मंज़र जान बूझ कर बनाया गया था, या ये एक तरह की गफ़लत और अनदेखापन था। व्हाट्सप्प और न्यूज़ चैनल्स ने भी लोगों को जागरूक और निर्भय बनाने के बजाय भय को खड़िया बनाकर एक घेरा खींच दिया था, जो ज़िंदा लोगों के लिए क़ैदख़ाना बन गया था।
दूसरी तरफ़ इंसानियत का ही एक और नज़ारा भी था। बहुतेरी स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था में सक्रिय योगदान कर रही थीं, और मुंबई में इन्हें तमाम नौजवान रंगकर्मी बिना किसी सरकारी अनुदान या मदद के चला रहे थे। अपनी उम्र और ब्लड शुगर की प्रॉब्लम को देखते हुए मैं इस तरह के काम में अपनी शारीरिक भागीदारी दर्ज़ नहीं कर सका था, लेकिन फ़ोन के ज़रिये मैं सभी के सम्पर्क में था। इन सहायता-कर्मी नौजवानों ने अपने रहने-सोने और खाने-पीने का इंतज़ाम भी वहीं पर कर लिया था, ताकि परिवार से दूरी बरक़रार रख सकें। सप्लाई और डिलिवरी स्टाफ़ और कुकिंग स्टाफ़ अलग-अलग यूनिट में काम कर रहे थे। बड़ी मुस्तैदी से इन रंग कर्मियों ने तक़रीबन पिच्चानबे दिनों तक दिन रात यह काम किया और दूर दराज़ बड़े-बूढ़े और अकेले पड़ गए कलाकारों और हर तरह के मजबूर लोगों को नियमित खाना पहुँचाया। जब भी किसी को सहायता की ज़रुरत पड़ी इन्होंने न दिन देखा न रात, और न ही कोई दूरी। उन्ही दिनों ईद भी पडी थी और पूरे तीस दिन इन लोगों ने सेहरी और इफ़्तारी लोगों के घर-घर पहुँचायी। यह सब यहाँ चन्द लाइनों में लिखना आसान है मगर इसके पीछे इन्सानियत के जज़्बे का जो इंजन लगा हुआ था उस जज़्बे को मैं सलाम करता हूँ।

ऐजाज़ व ऋचा/ Aijaz & Richa:
चुप के साथ आपने जो सफ़र किया उससे आपको और आपकी टीम को क्या हासिल हुआ है—कलात्मक रूप से, वैचारिक रूप से, सामुदायिक रूप से? या और किसी तरह से जो पाया उसके बारे में कुछ साझा कीजिये। क्या इस प्ले ने cross-border artistic collaborations के कुछ दरवाज़े खोले हैं? या कम-अज़-कम इस ख़्वाहिश को जनम दिया है कि हम एक दूसरे के साथ कला के ज़रिये जुड़ सकें?
तरुण/ Tarun:
चुप के साथ ईमानदार सफ़र करने का मतलब था नाटक की बारीकियों में उतरकर उसमें पसरी चुप्पियों के साथ इन्साफ़ करना। जैसा मैंने पहले कहा, इस नाटक में कहीं भी न तो किसी तंज़ीम का नाम लिया गया है, न किसी देश या प्रदेश का। किसी धार्मिक चिन्ह का तो किसी स्तर पर ज़िक्र भी नहीं, और मंच सज्जा के लिए भी कोई निर्देश नहीं है। ऐसे में स्तिथियों को स्पष्ट करने के लिए कलाकारों के मन में उपजते सवालों को समझने-समझाने का क्रम रोज़ चलता था, वो भी जीवन की घटनाओं से, या जो कुछ भी देखा-सुना-समझा-जिया था, उससे जोड़कर। यानी मामला सिर्फ़ लाइनें बोलने का नहीं, बल्कि अपने माहौल से नाटक के माहौल को जोड़ते हुए चुप्पियों के मायनों को सहजता से पिरोने का था। इस काम के लिए परख ग्रुप के सारे कलाकार हर वक़्त कमिटेड रहे और मुझे प्रेरित करते रहे और मैं उनके talent और समय का सदुपयोग करता रहा। दोनों ही तरफ से मथानी चल रही थी इसलिए मख्खन तो निकलना ही था। छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े सवालों को लगातार उठाते हुए हमने इस नाटक में उठाये गये मुद्दों की उपयोगिता और प्रासंगिकता को अपनी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी से जोड़ा और फिर उन पहलुओं को उभारने की लगातार कोशिश में लग गए। सफ़र के विषय पर ही अब कुछ दुसरे पहलुओं को भी छूना चाहता हूँ, जैसे ज़बान और परिवेश से जुड़े concepts—मसलन, ख़ुला।
शुरूआती दौर में हमारी दो स्त्री कलाकार बांगला ज़बान बोलने वाली थीं। एक का तो ज़्यादातर वक़्त बंगाल के बाहर कॉस्मोपॉलिटन शहरों में बीता है, लेकिन जो अम्मी का रोल कर रही थीं उनके उच्चारण में बांगला का पुट आता है, तो वो नाटक की जुबान के साथ ख़ुद को असहज महसूस कर रही थीं। परख थिएटर में जब तक कोई ख़ास वजह न हो तब तक हम किसी के प्रांतीय उच्चारण पर प्रश्न नहीं लगाते हैं। ज़बान के उच्चारण को लेकर सवाल लगाने को हम एक तरह की सामाजिक असमानता और मानसिक प्रताड़ना के समकक्ष देखते हैं जो एक कलाकार में हीन ग्रंथि का विकास कर सकता है। कलाकार के पास भाषा को लेकर जो कुछ भी है, और जैसा भी है, वह उनके व्यक्तित्व की पहचान है जिस पर उसको गर्व करने का अधिकार है। किसी भी ज़बान की महानता को थोपा जाना घातक होता है। अम्मी की तो पहले से ही बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं, वो भी हिंदी-उर्दू में, और हमारी कलाकार वैसे ही उनको लेकर थोड़ा घबराई रहती थीं, इसलिए उच्चारण को लेकर उन्हें दूसरे दबावों में डालना हमने उचित नहीं समझा। जब २०२२ से हम लोग स्टेज शो करने लगे हैं, तब से हमारे पास हिंदी-उर्दू बोलने वाली अम्मी और रबिया हैं इसलिए अब काफ़ी हद तक भाषा और उच्चारण का मसला हल हो चुका है।
हमारे इस नाटक बनाने के दौर में कुछ ऐसा हुआ कि हमसे जुड़ा कोई भी मुस्लिम कलाकार अपनी व्यस्तताओं की वजह से कोई मुख्य भूमिका निभाने में शिरकत नहीं कर सका। अतः नाटक में जब ख़ुला का ज़िक्र होता है तो उसके बारे में हिन्दू कलाकारों को कोई इल्म नहीं था और ना ही वे इसको अपनी धार्मिक मान्यताओं के नुक़्ता-ए-नज़र से समझ पा रहे थे। फिर हिन्दू परिवेश से निकले इन कलाकारों ने अपने क़रीबी मुस्लिम साथियों के साथ बैठकर अपनी-अपनी समझ को साफ़ किया और तभी अपने पूरे स्टान्स में और एटीट्यूड में, यानी जिस्मानी अंदाज़ों और बोलचाल के तौर तरीक़ों में, उसको आत्मसात कर पाए। वैसे भी हमारे मुल्कों में आजकल के बच्चों को अपने रिवाज और क़ायदे तब तक ज़्यादा मालूम नहीं होते हैं जब तक उनका किसी ख़ास परिस्थिति से आमना-सामना नहीं होता है। इसीलिए तो नाटक में भी ये बात आख़िर सलमान को किसी धर्म के जानकार से ही पूछनी पड़ी, जिसके बारे में जान कर रबिया सलमान के सामने भड़क जाती है।
नाटक की शुरूआत रबिया और सलमान के बीच की बातचीत से साथ होती है, जिसको देख कर मन में उत्सुकता जागती है: ये कैसे पति पत्नी हैं जिनके बीच कभी तो एक आत्मीय रिश्ता लगता है और कभी लगता है कि इनके दरम्यान कुछ उबल रहा है जिसका हमें अभी अंदाज़ नहीं है। उस पहले दृश्य के अंत में ज़ारा का आना, और रबिया और सलमान का इतनी रात को आपस में यों बात करना हालाँकि उसके लिये कोई ख़ास मायने नहीं रखता, फिर भी रबिया उसको सलमान से साथ अपनी मौजूदगी के लिए दलील देती सी लगती है—“चलो, मैं तो बस पानी पीने आयी थी,” जिससे नाटक के पहले सीन की यह एक लाइन हमारे ग़ौर करने के दायरे में ज़रूर आ जाती है कि आख़िर बच्ची के आगे रबिया को यह सफ़ाई देने की क्या ज़रुरत थी? लेकिन लेखक ने यह सब बहुत ही हलके हाथ से किया है। Subtlety इस प्ले में कमाल की है। चुप के साथ हमारा जो सफ़र रहा है वो दरअसल इन्हीं किरदारों की कहानियों और उनके बाहरी और अंदरूनी हालात को समझने का सफ़र रहा है। इसलिए मैं एक बार फिर से किरादरों की तरफ़ रुख़ करता हूँ।
ज़ारा से शुरू करें तो उस बच्ची की भूमिका ज़रा प्रयोगात्मक है जो इस ड्रामे को थोड़ा अलग तेवर देती है। वह किरदार आपको विषय से बाहर ले जाये बिना एक पल के लिए तनाव से राहत देता है और फिर वहीं वापस ले आता है। ज़ारा का आना-जाना और फ़ोन पर बातचीत करना वैसे ही हैं जैसे छोटे बच्चे खेल-खेल में किसी से बात करने का नाटक करते हैं या बातचीत करने भ्रम पैदा करते हैं। शायद इसीलिए अम्मी ज़ारा को बात करता देखने के बावजूद उसके डीटेल्स में नहीं जाती हैं, जबकि घर में अनजान कॉल्स को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। यहाँ तक कि जब वो नमाज़ पढ़ने भी जाती हैं तो रबिया को फ़ोन देकर जाती हैं इस ताकीद के साथ कि फ़ोन आये तो रिसीव करना।
मुझे पापा का ऊंचा सुनना भी ज़बरदस्त लगा। उनकी उम्र, शिथिलता, और उनका बहरापन उनके देश के प्रशासन जैसे मालूम देते हैं, क्योंकि उनकी शिथिल सरकार भी तो ऊंचा सुनती है। उनके हियरिंग ऐड का बार-बार भटक जाना, उनका बार-बार ऊँचा सुनना और बातों को दोहरा-दोहरा कर पूछना, उनका वार्ता को ख़त्म करना या टालना, मुद्दों से भागना और कभी-कभी मुद्दों को भटकाना और उठ कर चले जाना। ये सब जतलाता है कि परिवार का सबसे ख़ामोश, आहत, और चुप शायद यही इंसान है, जो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया है। अम्मी, रबिया और साद/ ज़ैन यों तो एक ही पलड़े पर झूमते दिखते हैं, फिर भी नाटक का पहला दृश्य और आखिरी दृश्य एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि रबिया और सलमान एक दिखते हुए भी दो मुख़तलिफ़ छोरों पर बने रहते हैं। जहाँ पहले दृश्य में सलमान अपनी उलझनों को लेकर रबिया पर दबाव बनाता हुआ दिखाई देता है, वहीं आख़िरी दृश्य में वो असमर्थ, असहाय और परिस्थितियों के सामने लाचार दिखाई देता है—जैसे रबिया के सवालों और उनसे पैदा हुए हालात के सामने हार गया हो।

पहले दृश्य में सलमान और रबिया के बीच के संवादों में कई बार दोहराव महसूस होता है जो शायद रिश्तों की नज़ाकत, औपचारिकता, और झिझक दर्शाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगले सीन के आते-आते अम्मी और पापा के साथ भी लाइन्स का रिपिटेशन पहले-पहल कुछ ज़्यादा लगता है। पापा को ऊँचा सुनाई देना इस रेपिटिशन की वजह नहीं है क्योंकि उनको आला लगा हुआ है। मैंने चुप के इस repetitive पहलू को एक तरह के बोरियत और अवसाद से जोड़ा जो इस तरह के उदास माहौल में रहते हुए पैदा होता है। यानी एक मनोवैज्ञानिक संक्रमण से उपजी हुई जीवन की परिस्थितियाँ और उन से पैदा हुई एक ग्रन्थि या एक तरह की आदत। भय और दबाव में अपनी बात कहने के पहले कोई इंसान जो भूमिका बनाता है वैसा ही प्रयास पापा करते दिखाई देते हैं। किसी भी बात को बार-बार कह-कह कर साफ़ करना, यानी वो अपने दिमाग़ को कुछ चीज़ें समझा ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा पहलू यह है कि सलमान पर आर्थिक निर्भरता की वजह से उनकी एक मजबूरी भी है और शायद उसी के चलते पापा सलमान से बात करने से कतराते हैं और बेटे से जो बेहद ज़रूरी बात करवाने के लिए उनकी बीवी ज़िद पर अड़ी हैं, उस बात को उठाने वाली स्थितियों से ख़ुद को बचाते-से दिखते हैं।
पहले दृश्य में सलमान और रबिया के बीच के संवादों में कई बार दोहराव महसूस होता है जो शायद रिश्तों की नज़ाकत, औपचारिकता, और झिझक दर्शाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगले सीन के आते-आते अम्मी और पापा के साथ भी लाइन्स का रिपिटेशन पहले-पहल कुछ ज़्यादा लगता है। पापा को ऊँचा सुनाई देना इस रेपिटिशन की वजह नहीं है क्योंकि उनको आला लगा हुआ है। मैंने चुप के इस repetitive पहलू को एक तरह के बोरियत और अवसाद से जोड़ा जो इस तरह के उदास माहौल में रहते हुए पैदा होता है। यानी एक मनोवैज्ञानिक संक्रमण से उपजी हुई जीवन की परिस्थितियाँ और उन से पैदा हुई एक ग्रन्थि या एक तरह की आदत। भय और दबाव में अपनी बात कहने के पहले कोई इंसान जो भूमिका बनाता है वैसा ही प्रयास पापा करते दिखाई देते हैं। किसी भी बात को बार-बार कह-कह कर साफ़ करना, यानी वो अपने दिमाग़ को कुछ चीज़ें समझा ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा पहलू यह है कि सलमान पर आर्थिक निर्भरता की वजह से उनकी एक मजबूरी भी है और शायद उसी के चलते पापा सलमान से बात करने से कतराते हैं और बेटे से जो बेहद ज़रूरी बात करवाने के लिए उनकी बीवी ज़िद पर अड़ी हैं, उस बात को उठाने वाली स्थितियों से ख़ुद को बचाते-से दिखते हैं।
पापा जिनकी उम्र इस वक़्त सत्तर साल की है, कर्ज़दार हैं, और उनके क़र्ज़ की भरपाई उनका बेटा सलमान कर रहा है, वही जो घर के सारे ख़र्च भी उठा रहा है। पापा का अपना निजी घर नहीं है। उनके छोटे भाई ने उनके साथ कोई बड़ा धोखा किया था जिसकी वजह से उनके कारोबार में ख़ासा नुक़सान भी हुआ है। फिर भी उन्होंने अपने उसी भाई की बेटी के साथ साद/ ज़ैन का निकाह कर दिया। चाहे जो भी मजबूरियां रही हों, और जो भी उनको मुनासिब लगा हो ख़ासकर साद/ ज़ैन के चाल चलन को देखते हुए। क्योंकि नाटक में कई बार सलमान और अम्मी के बीच की बातों में ज़िक्र मिलता है कि साद/ ज़ैन की रबिया से शादी किसी-न-किसी तरह का समझौता ही थी जिसको रबिया भी निभा रही है। पापा इस दबाव को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। घर के नाज़ुक आर्थिक माहौल को भी वो गहराई से समझते हैं। ऊपर से छोटे बेटे की ग़ैर मौजूदगी का ग़म तो है ही, जिसको वो अलफ़ाज़ से ज़ाहिर न करके अपनी हरकतों से ज़ाहिर करते हैं। कभी-कभी लगता है कि वो शायद मसले को टालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मगर नाटक के पाँचवें दृश्य के आते-आते उनका बार-बार दरवाज़े पर किसी के आने की आहट पर उठ कर जाना उनकी मानसिक स्थिति का इज़हार करता है। और फिर उनका एक ख़ामोशी इख़्तियार कर लेना और डॉक्टर का यह कहना कि उनके न बोलने की वजह कोई बीमारी नहीं है, बस वो बोलना नहीं चाहते हैं। इन सबसे यही लगता है कि वो सलमान और अपनी बीवी के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहते हैं। यानी, मौजूदा हालात में पापा के ऊपर दो तरफ़ा वार चल रहे हैं—एक तरफ़ से आर्थिक तंगी, और दूसरी तरफ़ पत्नी का यह तय कर लेना कि उसे अपने गुमशुदा बेटे के लिए इन्साफ़ चाहिए।
अम्मी इस नाटक की एक मज़बूत किरदार हैं और नाटक का हर किरदार पूरी तरह से उनके इर्द गिर्द बंधा हुआ है। वह बड़ी तेज़ तर्रार घरवाली हैं और घर में उनकी अनकही हुकूमत चलती है। पति को धौंसिया कर अपनी मन मर्ज़ी का करवाने वाली कला में उन्हें पूरी महारत हासिल है। साद/ ज़ैन की ग़ैर मौजूदगी और उसकी शादी तक के लिए वही ज़िम्मेदार लगती हैं और अपने छोटे बेटे को हर मोड़ पर पूरी तरह शह देती या बचाती हुई नज़र आती हैं। आज घर के जो हालात हैं उनकी एक वजह उस गुमशुदा बेटे के लिए उनका लाड़-प्यार भी है, जिसको वो नकार नहीं पाती हैं। इस पूरे नाटक में उनका धाकड़पन अगर कोई नकार सकता है तो वो है उन्हीं का बड़ा बेटा, सलमान। पापा यह बात जानते हैं, इसीलिए जब वो अम्मी के बहुत ज़ोर देने पर सलमान से बात करने के लिए राज़ी भी होते हैं तो वो अम्मी से बार-बार अपने कमरे में जाने का इसरार करते दिखाई देते हैं। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि बीवी से साफ़-साफ़ कह सकें, “आप अंदर जाइए, तब मैं बात करूँगा।”
पूरे नाटक में जहाँ अम्मी धीरे-धीरे अपनी गिरफ़्त बढ़ाती चली जाती हैं, वहीं पापा एक कमज़ोर, दबे, और टूटे हुए किरदार बनते चले जाते हैं। मियाँ-बीवी के बीच तक़रीबन दस साल का फ़ासला है और दोनों बरसों से एक साथ रहते हुए एक दूसरे में काफ़ी गुंथे हुए भी हैं। बड़ा बेटा सलमान बाप का लिहाज़ करता है और उनके सामने लगभग तमीज़ के दायरे में रहता है, लेकिन उसे अफ़सोस है कि उसके पापा उसकी बेटी ज़ारा की फ़िक्र नहीं करते, जबकि सलमान ख़ुद इस घर के ख़र्च और अपने बाप का कर्ज़ा तक उतारने में कभी पीछे नहीं हटा है।
रबिया वो औरत है जिसका अपना पति शादी के एक हफ़्ते बाद से ग़ायब है। उसे एहसास है कि उसके अपने वालिद ने पापा के क़ारोबार में ख़ासा माली नुक़सान किया है। वो अपनी बड़ी अम्मी और पापा को अब इससे ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती है, इसीलिये वो इस घर में रहकर इन सभी की ख़िदमत कर रही है। सलमान की बीवी का इंतक़ाल हो चुका है और उसकी नौ साल की बेटी ज़ारा की देखभाल भी रबिया ही कर रही है। साद/ ज़ैन के चले जाने के बाद ज़ारा उसे तमाम चीज़ों में उलझाए रखती है। ज़ारा अपनी चची के साथ ही रहती-सोती, उठती-बैठती है क्योंकि उस नन्ही जान का भी और कोई आसरा नहीं है। रबिया की जिस्मानी ज़रूरतें भी हैं, जिनका होना और जिनका पूरा किया जाना दोनों लाज़मी है। रबिया और सलमान मिलकर अपनी इन ज़रूरतों को चोरी-छुपे वक़्त बे-वक़्त पूरा भी करते हैं। चोरी छुपे ऐसे रिश्ते को निभाना, और वो भी एक ही छत के नीचे, दोनों के लिये आसान नहीं है। उसके रास्ते बनाते हुए सलमान रबिया को लेकर कहीं दूर चले जाने के गुंताड़े बुनता रहता है, जो हम नाटक के पहले दृश्य में ही देखते हैं। रबिया इस सब में बहुत बुरी तरह उलझी हुई है कि वो करे तो क्या करे? साथ ही, वह अपने बड़े पापा और बड़ी अम्मी को और दुःख नहीं देना चाहती।

सलमान डॉक्यूमेंटरी फ़िल्में बनाता है। उसको जो काम जहाँ कहीं से भी मिलता है, वो करता है। उसके हाव-भावों में एक तरह का समझौता दिखाई देता है। जब अम्मी उलाहना देती हैं कि अच्छा, तुम ‘उन्हीं’ लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो उसे सिरे से नकारते हुए वह कहता है कि आप अपने काम से काम रखें। वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेना चाहता है कि रबिया और ज़ारा को लेकर दुबई शिफ़्ट हो सके। वह घर की माली हालत को संभालते हुए पूरे परिवार की तमाम ज़िम्मेदारियों को भी बख़ूबी उठाने में लगा रहता है। उसे अम्मी और पापा को आरामदेह ज़िंदगी देनी है मगर अब उसके मन में साद/ ज़ैन के साथ हमदर्दी दिखाने की कोई तमन्ना नहीं है। उसके घरवाले अभी भी जिस तरह उसके भाई के लौटने की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, वह रवैया उसे नागवार गुज़रता है। पापा यों तो उससे हर ज़िम्मेदारी को पूरा करने की उम्मीद रखते हैं, मगर सलमान उनके दिल में अपने, रबिया, और ज़ारा के लिए कोई जगह नहीं देख पाता। वो चाहता है कि लोग समझ लें कि साद/ ज़ैन अब एक बीता हुआ लम्हा है जिसे सबके हित में पूरी तरह भुला देना ही ठीक होगा। साद/ ज़ैन की वजह से उसके पास कभी एक धमकी भरा मैसेज आया था, उसको ही आधार बना कर और ज़ारा का वास्ता देकर वह सबको ख़ामोश कर देना चाहता है, ताकि वह रबिया के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। वो जहाँ एक तरफ़ अम्मी और पापा से तल्ख़ है वहीं दूसरी तरफ़ वो रबिया के रूखे तौर-तरीक़ों और परिवार वालों को लेकर उसके संवेदनात्मक रवैये से भी नाख़ुश है। सलमान ने एक और भी ड्रामा खड़ा किया हुआ है कि ज़ारा की टीचर ने उसे फ़ोन करके साद के बारे में पूछा था। जब रबिया कहती है, “मैं टीचर से बात करती हूँ”, तो वह उसे उलाहना देता है कि “इस घर में तो किसी से कोई बात करता नहीं, आप टीचर से बात करेंगी?” वही सलमान दुबई से लौटने वाले दृश्य में ज़ारा के स्कूल का फ़ोन नंबर लेने के लिए कितनी हड़बड़ी दिखाता है, यानी उसके पास स्कूल का कोई भी नंबर है ही नहीं, न ही उसे ज़ारा की क्लास और सेक्शन मालूम हैं। ये सब ज़ारा और उसके स्कूली मामलों की तरफ़ से उसकी पूरी नज़रअंदाज़गी का मुज़ाहिरा करते हैं, और वह इन सब चीज़ों को रबिया पर ही छोड़ कर सुकून महसूस करता है।
साद/ ज़ैन के लिए माँ का कोमल कोना सलमान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। वह अपनी माँ को आहत करने के मक़सद से कहता है, “आप नहीं जानती थीं कि आपका वो बेटा शादी नहीं करना चाहता था।” ये जुमला अपने आप में कई सवाल खड़े करता है साद/ ज़ैन की यौनिकता के बारे में। या फिर सलमान का इशारा अपने भाई की उन हरकतों की तरफ़ है जिनमें हो सकता है सलमान भी कभी मुल्लविस रहा हो। एक तरह से सलमान अपनी माँ पर इलज़ाम लगाता है कि उन्होंने यह सब जानते-बूझते हुए और उन “नाजायज़” चीज़ों से अपने छोटे बेटे का ध्यान हटाने के लिए ही रबिया का इस्तेमाल किया, क्योंकि रबिया अपने वालिद के कारनामों की वजह से पारिवारक दबाव में थी। चूँकि रबिया का कोई सहारा नहीं था इसीलिए उसके वालिदैन ने उसकी शादी साद/ ज़ैन के साथ बड़ी आसानी से कर दी। साद/ ज़ैन की जो भी मजबूरियाँ या इरादे रहे हों, उनकी ख़बर उसने किसी को भी नहीं होने दी, और शादी के एक हफ़्ते बाद ही वह ग़ायब हो गया, या कर दिया गया।

Courtesy: Parakh Theatre Archive.
चुप के प्रदर्शनों के साथ परख का सफ़र देखें तो कोविड के दौर में हमने आमंत्रित दर्शकों के साथ चार ऑनलाइन शो रखे थे, जिनमें पहला शो फ़वाद और ऋचा के लिए रखा था। फ़वाद, यानी हमारे नाटककार, कराची में थे, और ऋचा, जो हमारी प्रक्रिया और परख थिएटर ग्रुप का अभिन्न हिस्सा हैं और जिनके बिना हम इस नाटक तक पहुँच नहीं पाते, मिनिसोटा में क़ैद थीं। हम दोनों की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। दोनों को ही काम बहुत पसंद आया, और फ़वाद ने अभिनेताओं के साथ अपने कुछ अनुभव भी साझा किये।अपने कराची के प्रोडक्शन में उन्होंने सलमान की भूमिका भी निभाई थी, सो उन्होंने अपने वहां के अनुभवों और दुश्वारियों का भी ज़िक्र किया। उस मुलाक़ात के साथ ही पूरी टीम का फ़वाद के साथ एक गहरा रिश्ता बनता महसूस हुआ।
हम सब जानते हैं कि मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और श्रीलंका की सांस्कृतिक भूमि और संस्कार एक दूसरे में गुंथे हुए हैं, हाँलाँकि हमें तकसीम और उसके बाद के हालात ने अच्छी तरह सिखाया है कि राज्यों की सीमाएं देशीय और वैश्विक राजनीति का हिस्सा हैं और नफ़रतों से वोट बनते हैं, जंगें लड़ी जाती हैं, और मुनाफ़े कमाए जाते हैं। फिर भी, हमारे सोचने और महसूस करने के ढंग, हमारे आचार-विचार, रीति-रिवाज, और बोलचाल की ज़बानों को किसी भी क़िस्म का बंटवारा बाँट नहीं सका है। गीत, गज़ल, साहित्य, नाटक, फ़िल्में, हॉकी, क्रिकेट हमारी साझी संस्कृति और हमारे रूहानी जुड़ाव का हिस्सा हैं, जिन्होंने हमें एक-दूसरे का मुरीद बना कर रखा हुआ है। मैं २००३ में एक नाटक “सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक” के साथ लाहौर के वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल में गया था। बड़ा यादगार अनुभव था। मेरी परवरिश लखनऊ में हुई और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, इसलिए ज़बानी ताल्लुक़ तो था ही। मुझे एक पल को भी नहीं लगा कि मैं किसी ग़ैर मुल्क में हूँ। पाकिस्तान की अवाम का प्यार और ख़ुलूस देखते ही बनता था। अवाम के नुक़्ता-ए-नज़र से देखें तो अब भी लाहौर में फैज़ की याद में हिन्दुस्तान के तमाम साहित्यकार मेला लगाते हैं, और पाकिस्तानी कलाकारों, गायकों, और कॉमीडियंस की हमारे हिन्दुस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ख़ासी मौजूदगी रही है, हाँलाँकि इधर सीमाओं के आर-पार तनातनी बढ़ी हुई है।
चुप ने थोपी हुई हर सीमा के आर-पार एक-दूसरे के लेखन और काम को क़रीब से देखने-समझने के जज़्बे और प्रतिबद्धता को बढ़ाया है। रंगमंच तमाम सांस्कृतिक विधाओं को साथ लाकर जादू करता है। थिएटर हर हाल में लोगों को क़रीब लाता है, चाहे वह किसी मंच पर हो या किसी नुक्कड़ पर। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस क़रीबियत को सार्थक रिश्तों में बदल कर समाज को दिशा देने का काम कैसे करें। फ़वाद ने जिस विश्वास के साथ ऋचा को चुप की यह स्क्रिप्ट दी और उसके बाद इसके हर पहलू पर अपनी बेबाक़ राय दी, और अब AGITATE! के इस वॉल्यूम ने जिस तरह सोचने और लिखने का न्योता दिया—इस पूरे सफ़र ने बार-बार यही महसूस करवाया है कि क्रॉस-बॉर्डर क्रिएटिविटी गहरे भरोसे और मोहब्बतों की खेती है—इसके जितने बीज हम बोते चलेंगे, उतने ही ये सिलसिले लहलहाते रहेंगे।
अक्सर हम भौगोलिक सीमाओं में ही उलझ कर रह जाते हैं, जबकि ज़ेहनी और दिली सीमाओं को छूना और पार करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी, कठिन, और मुसलसल करते रहने वाला काम है। हमारे मुल्कों की सरकारी नीतियाँ चाहे कितने ही खेल खेलें और सर्मायादार लोग चाहे कितनी ही खाइयाँ बनायें, हमें इनसे बिना घबराये एक दूसरे से समझते-सीखते-जुड़ते हुए दरारें भरने का काम जारी रखना होगा। बिगड़ी हुई राहों से राहें तब तक निकलती रहेंगी जब तक हम नई राहें बनाने में लगे रहेंगे। हर मोहब्बत को हमेशा जज़्बे और भरोसे का ईंधन चाहिए, तो यह मोहब्बत भी कभी न ख़त्म होने वाला सफ़र और प्रतिबद्धता है। सच्चाई तो यह है कि इसके बिना हमारी और हमारे मुल्कों की रूहें ज़िन्दा ही नहीं रह पायेंगी।
चुप की यात्रा में जो कलाकार मेरे साथ कंधे से कन्धा मिलाकर चले उन सभी का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। माधुरी संजीव, प्रियंका कौल, अपर्णा घोषाल, वीणा कृष्णन, पूर्णिमा खड़गा, चित्रा मोहन, मनोज सिंह कैड़ा, मनीष टंडन, नोयोनिता लोध, निधि अस्थाना हुसैन, सुदीप्ता सिंह, ज़ेबा हुसैन, शिफ़ा शेख, रिया शर्मा, निखिल जरूहार, अचल यादव, गौरव गुप्ता, अली जाफ़री, ऋत्विक चौधरी, हार्दिक सिंह राठौर, ममता सिंह, शेखर सोम, सत्यदेव कुमार, टेफ़्ला स्टूडियो, तथा क्रिएटिव अड्डा के साथी: आप सभी के बिना यह यात्रा जो चली और चल रही है, वह अधूरी और अकेली होती। आप सभी ने हर वक़्त मेरा साथ दिया और इस सफ़र को लगातार हिम्मत और नए मायने दिए। खेल जारी है!
Suggested citation:
Kumar, T., A. Aijaz, & R. Nagar. 2024. “Carrying Silences Across Borders: Tarun Kumar Speaks with Abdul Aijaz and Richa Nagar | चुप्पियाँ और सरहदें: तरुण कुमार के साथ अब्दुल ऐजाज़ और ऋचा नागर की बातचीत.” In Eds. Richa Nagar, Abdul Aijaz, and Nithya Rajan, Special Volume on “Ecologies of Violence and Haunting: Listening to Chup,” AGITATE! 5: https://agitatejournal.org/article/carrying-silences-across-borders-tarun-kumar-speaks-with-abdul-aijaz-and-richa-nagar/
Article by: